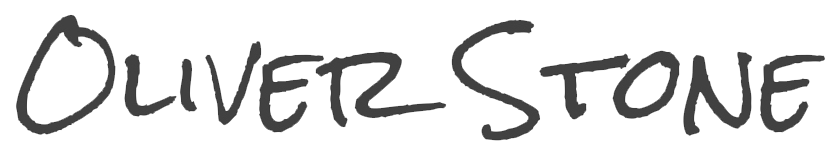Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

-डॉ. मयंक चतुर्वेदी
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर किसी शैक्षणिक उपलब्धि, शोध या बौद्धिक योगदान के लिए नहीं, आपत्तिजनक नारेबाजी, उग्र मानसिकता और लोकतंत्र विरोधी आचरण के कारण राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध लगाए गए उत्तेजक और हिंसक नारे इस बात का प्रमाण हैं कि जेएनयू में लंबे समय से पनप रही वामपंथी राजनीति अब असहमति की सीमा लांघ चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इसे जानबूझकर किया गया कृत्य बताते हुए पुलिस से गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग करना भी आज यह बता रहा है कि वर्षों से चले आ रहे वैचारिक अराजकता के विरुद्ध एक अनिवार्य हस्तक्षेप अब अनिवार्य हो गया है।
वामपंथी सोच का सबसे बड़ा और घातक प्रभाव यह रहा है कि उसने भारत के विकास को हमेशा संदेह और शत्रुता की दृष्टि से देखा। आर्थिक सुधार, बुनियादी ढांचे का विस्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णय, आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कदम या सामाजिक सुधार, हर पहल को ‘फासीवाद’, ‘राज्य दमन’ या ‘कॉरपोरेट साजिश’ बताकर खारिज करने की प्रवृत्ति लगातार देखने को मिलती है। जेएनयू में फीस वृद्धि, अनुच्छेद 370, सीएए या अन्य किसी भी विषय को लेकर आंदोलन का तरीका हमेशा एक जैसा रहा है। पढ़ाई ठप करो, परीक्षाएं रोक दो, रजिस्ट्रेशन बाधित करो और सामान्य छात्रों को बंधक बना लो।
पिछले महीनों में यही रणनीति खुलकर सामने आई। सेमेस्टर परीक्षाओं को बाधित किया गया, छात्रों को कक्षाओं में जाने से रोका गया, विश्वविद्यालय के मुख्य भवन पर कब्जा किया गया और जब छात्रों ने धमकियों के बावजूद रजिस्ट्रेशन शुरू किया तो सर्वर रूम में घुसकर इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसके बाद भी जब अधिकांश छात्रों ने वैकल्पिक माध्यमों से पंजीकरण कर लिया, तो उन पर डंडों, रॉड और धारदार हथियारों से हमला किया गया। यह सब किसी छात्र आंदोलन का स्वरूप नहीं हो सकता है, ये सीधे तौर पर संगठित हिंसा और वर्चस्व की राजनीति है।
कहना होगा कि यह घटना किसी एक दिन, एक समूह या एक प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है। यह उस वैचारिक परंपरा का नवीन अध्याय है, जिसने जेएनयू को शिक्षा और शोध के केंद्र से अधिक एक राजनीतिक अखाड़े में बदल दिया है। साल 1969 में स्थापना के बाद से ही वामपंथी छात्र संगठनों और उनके वैचारिक समर्थकों का इस विश्वविद्यालय पर लगभग एकाधिकार रहा है। इस आधिपत्य का परिणाम यह हुआ कि कैंपस में सहमति और असहमति को तार्किकता की कसौटी पर नहीं पखरा जाता। आज भी यहां हिंसा, धमकी और दबाव के जरिए तर्कों को कुचला जा रहा है।
साल 1983 में तो हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि पूरे एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय को बंद करना पड़ा था। उस समय न तो किसी गैर वामपंथी सरकार का दबाव था और न ही किसी वैकल्पिक विचारधारा का प्रभाव। तत्कालीन कुलपति पीएन श्रीवास्तव के घर में घुसकर की गई तोड़फोड़, लूट और शिक्षकों के साथ की गई बर्बरता इस बात का प्रमाण थी कि हिंसा वामपंथी राजनीति की आकस्मिक प्रतिक्रिया न होकर उसकी अंतर्निहित प्रवृत्ति है। उस दौर में भी वामपंथी शिक्षकों की भूमिका छात्रों को उकसाने और हिंसा की योजना बनाने में संदिग्ध रहती रही। इसके बाद के दशकों में यह सिलसिला और अधिक उग्र होता गया।
साल 1990 और 2000 के दशक में जेएनयू परिसर में हुई कई घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया। कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान समर्थक कविताओं का मंचन, भारतीय सैनिकों द्वारा विरोध किए जाने पर उनके साथ की गई निर्मम मारपीट, साल 2005 में प्रधानमंत्री के आगमन पर हुआ उपद्रव, साल 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवानों के बलिदान पर कथित जश्न, साल 2013 में दुर्गा और हिंदू आस्था के अपमान से जुड़ा महिषासुर दिवस और साल 2016 में अफजल गुरु की बरसी पर भारत विरोधी नारे, ऐसे अनकों देश विरोध के कृत्य यहां आए दिन देखने में आते हैं, ये सभी घटनाएं एक ही वैचारिक धारा की निरंतरता को दर्शाती हैं और बताते हैं कि वामपंथ भारत के लिए कितना विनाशक साबित हुआ है।
हर बार देखने में यही आया है कि इन नारों और कार्यक्रमों का निशाना सरकार की नीतियों के साथ भारत की एकता और अखंडता, उसकी सांस्कृतिक आस्था और उसका संविधान लगातार इस राजनीति के केंद्र में रहे हैं। ‘आइन ए हिंदुस्तान का मंजूर नहीं’ जैसे नारे यह स्पष्ट करते हैं कि असहमति की आड़ में संवैधानिक व्यवस्था को ही अस्वीकार करने की मानसिकता जेएनयू में विकसित की जा रही है। इस पर भी आश्चर्य यह है कि जो कुछ यहां घट रहा है, वह लोकतंत्र और अभिव्यक्ति के साथ उसी संविधान की आड़ लेकर किया जाता है, जिसके विरोध में यहां नारे लगते हैं।
ताजा घटनाक्रम में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद जेएनयू में ‘मोदी शाह की कब्र खुदेगी’ जैसे नारे लगना इस तथ्य को उजागर करता है कि वामपंथी राजनीति अब न्यायपालिका के निर्णयों को भी खुलेआम चुनौती देने लगी है। कहना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इसे सुप्रीम कोर्ट की प्रत्यक्ष अवमानना बताया जाना बिल्कुल सही है। यह कोई भावनात्मक या अनजाने में हुई अभिव्यक्ति नहीं है, ये तो सामने से सत्ता और राज्य के विरुद्ध हिंसक भाषा को सामान्य बनाने का प्रयास है।
हाल के दिनों में जाति आधारित नारे लिखे जाने और ब्राह्मणों तथा अगड़ी जातियों को खुलेआम धमकियां देने की घटनाएं इस राजनीति के एक और खतरनाक पहलू को उजागर करती हैं। पहचान की राजनीति को हथियार बनाकर समाज में विभाजन पैदा करना और डर का माहौल बनाना वामपंथी राजनीति की पुरानी रणनीति रही है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि जेएनयू केंद्रित यह वामपंथी राजनीति अक्सर नक्सली, माओवादी, जिहादी और अलगाववादी विचारों से वैचारिक साम्यता दिखाती है। शहरी बुद्धिजीवी नेटवर्क, विश्वविद्यालयी मंच और सशस्त्र संघर्ष, इन तीनों के बीच संबंधों को बार बार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दंतेवाड़ा और सुकमा जैसे नरसंहारों पर जिस प्रकार के बयान और औचित्यकरण सामने आते रहे हैं, वे इस वैचारिक गठजोड़ को उजागर करने के लिए पर्याप्त हैं।
लोकतंत्र में असहमति का स्वागत हमेशा से रहा है, किंतु इसका अर्थ हिंसा, धमकी और राष्ट्र विरोध कदापि नहीं हो सकता। विश्वविद्यालयों का उद्देश्य प्रश्न उठाना है, वह भी उन उत्तरों की खोज में, जिन्हें जानना लोक के विकास एवं परमार्थ के लिए आवश्यक है, नकि समाज और राष्ट्र को तोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों (शिक्षा के मंदिरों) का उपयोग किया जाए। जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को यदि कुछ वामपंथी समूह अपने अस्तित्व के संकट से उबरने के लिए प्रयोगशाला बना रहे हैं तब फिर इसे रोकना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ये सोच पूरे देश की बौद्धिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए संकट पैदा करती है। वस्तुत: हमें सदैव याद रखना चाहिए कि भारत का भविष्य उन शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित है जहां ज्ञान, अनुशासन और राष्ट्रबोध साथ-साथ चल रहे हैं, न कि वहां जहां विचारधारा के नाम पर हिंसा और नफरत को वैध ठहराया जाए।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी