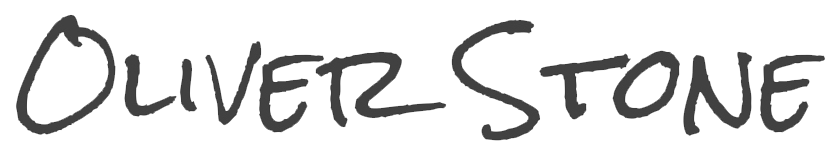Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

-कैलाश चन्द्र
भारत का लोकतंत्र अपनी विविधता, मतभिन्नता और खुली बहस की परंपरा के कारण विश्व में विशिष्ट रहा है। किंतु पिछले दो दशकों में एक ऐसी वैचारिक धारा विकसित हुई है, जिसने विश्वविद्यालयों, वामपंथी छात्र संगठनों, शहरी बुद्धिजीवी समूहों और माओवादी हिंसा को व्यापक वैचारिक सूत्र में पिरो दिया है। यह विमर्श केवल छात्र-राजनीति या असहमति तक सीमित नहीं; यह राज्य-विरोध, पहचान की राजनीति, ‘क्रांतिकारी प्रतिरोध’ की संस्कृति और अंततः माओवादी सशस्त्र संघर्ष तक फैला सुनियोजित नैरेटिव बन चुका है।
सबसे स्पष्ट उदाहरण दिल्ली के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय- जेएनयू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया तथा हैदराबाद एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय हैं, जहाँ विमर्श का झुकाव धीरे-धीरे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हटकर एक प्रकार के वैचारिक अराजकवाद की ओर दिखाई देता है। जेएनयू में एसएफआई, एआईएसए, डीएसएफ, डीएसयू जैसे वामपंथी छात्र संगठनों ने बीते वर्षों में न केवल वर्ग-संघर्ष के अपने पुराने नारे को पुनर्जीवित किया बल्कि राज्य, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खुलेआम चुनौती देने वाले आंदोलन खड़े किए।
साल 2016 में अफजल गुरु की फाँसी के विरोध में लगे “भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी” और “पाकिस्तान जिंदाबाद” जैसे नारे विश्वविद्यालयी राजनीति को निर्णायक मोड़ देने वाले सिद्ध हुए। यह सिर्फ एक छात्र-प्रदर्शन भर नहीं था; यह राष्ट्र-राज्य और न्यायिक संरचना को अवैध ठहराने वाले वैचारिक उभार का संकेत था, जिसमें अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के प्रति सहानुभूति जताई गई और भारतीय न्याय व्यवस्था को “कातिल” बताने की मुहिम चली।
इसी क्रम की अगली कड़ी जनवरी 2026 में तब उभरी, जब उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएँ खारिज होने पर जेएनयू में “मोदी–शाह की कब्र खुदेगी” जैसे हिंसक-उन्मादी नारे लगे। ये नारे लोकतांत्रिक असहमति से कहीं आगे बढ़कर हिंसक क्रांति की विचारधारा को वैधता प्रदान करते दिखे। एबीवीपी तथा अन्य समूहों द्वारा इसे राष्ट्र-विरोधी गतिविधि बताया जाना स्वाभाविक था; विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज करने से यह स्पष्ट हुआ कि परिसर केवल बहस के मंच नहीं रह गए बल्कि वैचारिक युद्धभूमि में बदल रहे हैं।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सीएए-एनआरसी आंदोलन के बाद तो ‘प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स’ का एक नया मॉडल विकसित हुआ- जहाँ सड़क, सोशल मीडिया और विश्वविद्यालय परिसर मिलकर ऐसा नैरेटिव गढ़ते हैं जिसमें अल्पसंख्यक अधिकार, राज्य दमन और उदार-वामपंथी विमर्श एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। यहाँ भी वही तर्क- फासीवाद, पुलिस-राज, राज्य-आतंक- प्रमुखता से उभरे, जो माओवादी अपने हिंसक संघर्ष को उचित ठहराने के लिए दशकों से उपयोग करते आए हैं।
यही वैचारिक साम्यता भारत के आदिवासी अंचलों में फैली माओवादी हिंसा को विश्वविद्यालयी विमर्श से जोड़ती है। साल 2010 के दंतेवाड़ा नरसंहार, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवानों की मौत हुई, कुछ वामपंथी बुद्धिजीवियों ने इसे “ऑपरेशन ग्रीन हंट का प्रतिकार” कहकर उचित ठहराने का प्रयास किया। इसी प्रकार साल 2021 में सुकमा-बीजापुर में 22 जवानों की हत्या और इन घटनाओं में माओवादी कमांडर मदवी हिड़मा की भूमिका यह प्रमाण है कि विचार जब हथियारों के साथ घुल-मिल जाते हैं, तो वह राष्ट्र और उसके रक्षकों पर प्रहार के रूप में सामने आते हैं।
साल 2025 में हिड़मा और बसवराजू जैसे शीर्ष माओवादी नेताओं के मारे जाने के बाद भी शहरी नक्सली नेटवर्क सक्रिय रहा। उसी वर्ष दिल्ली के प्रदूषण-विरोधी प्रदर्शनों में मदवी हिड़मा के समर्थन में नारे और बिरसा मुंडा की छवि के साथ हिड़मा के पोस्टर लगाना यह दर्शाता है कि शहरी नेटवर्क न केवल ग्रामीण हिंसा का समर्थन करते हैं बल्कि आदिवासी प्रतीकों को माओवादी हिंसा के औचित्य के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति अपनाते हैं।
इन घटनाओं से स्पष्ट है कि भारत में वामपंथी छात्र राजनीति अब सिर्फ परिसर-गत मुद्दों का विस्तार नहीं रह गई; यह राष्ट्रीय राजनीति से लेकर सशस्त्र माओवादी संघर्ष तक फैला बड़ा वैचारिक मोर्चा है। न्यायपालिका के निर्णयों- अफजल गुरु, बुरहान वानी आदि के विरुद्ध जिस आक्रोश और “प्रतिरोध” का नैरेटिव खड़ा किया गया, वह वही समूह कर रहे हैं जो लगातार राज्य की नैतिक वैधता को ही संदेह के घेरे में रखते हैं।
“भारत तेरे टुकड़े होंगे” और प्रधानमंत्री–गृहमंत्री के लिए खुलेआम हिंसक धमकियाँ, लोकतांत्रिक असहमति नहीं बल्कि अराजकता की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। इस वैचारिक तंत्र के भीतर मार्क्सवादी समूहों, इस्लामी कट्टरपंथी धाराओं, माओवादी नेटवर्क और कुछ विदेशी मिशनरी संगठनों की गतिविधियों का घालमेल एक प्रकार के वैचारिक ‘कॉकटेल मॉडल’ के रूप में उभर रहा है- जिसका लक्ष्य भारत की एकता को कमजोर करना, समाज में विभाजन पैदा करना और राज्य-व्यवस्था को चुनौती देना है।
पूर्वोत्तर भारत को ‘चिकन नेक’ क्षेत्र में विभाजित कर अलग करने की खुली वकालत करने वाले समूहों को भी लंबे समय से विश्वविद्यालय परिसर वैचारिक ऊर्जा प्रदान करते रहे हैं। यदि ऐसे शैक्षणिक केंद्र और शहरी नेटवर्क अनियंत्रित रहे, तो आने वाले समय में यही संस्थान वैश्विक मंच पर भारत की पहचान को अराजकता, हिंसा और पत्थरबाज़ी के प्रतीकों में बदल सकते हैं।
अंततः प्रश्न यह नहीं कि असहमति होनी चाहिए या नहीं- असहमति लोकतंत्र की आत्मा है। प्रश्न यह है कि क्या असहमति की आड़ में राष्ट्र-विरोध, हिंसा और सशस्त्र संघर्ष का समर्थन दिया जा सकता है? क्या विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र बने रहेंगे या राजनीतिक रणभूमि बन जाएंगे? क्या भारतीय वामपंथ माओवादी हिंसा से स्वयं को स्पष्ट रूप से अलग कर अपनी वैधानिक भूमिका सिद्ध करेगा? क्या भारत अपनी शिक्षा संस्थाओं को विदेशी हस्तक्षेप, वैचारिक प्रदूषण और उग्रवाद के बढ़ते प्रभाव से सुरक्षित रख सकेगा? भारत का भविष्य इन्हीं निर्णायक प्रश्नों के उत्तरों में निहित है।
(लेखक, वरिष्ठ स्तम्भकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी