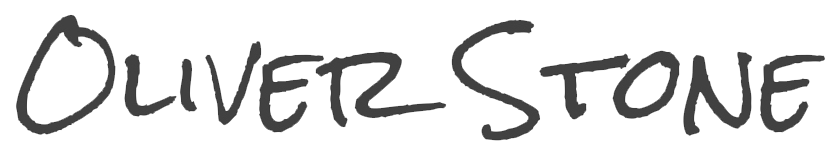Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

-कैलाश चन्द्र
दंतेवाड़ा में हाल ही में भाकपा (माओवादी) प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़े 37 नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ, जिनमें कई उच्च इनामी भी शामिल थे। निश्चित ही यह उस वैचारिक ढांचे के विघटन का संकेत है जिसने दशकों तक जनजाति समाज को भय और हिंसा में जकड़े रखा। पिछले कुछ महीनों में यह प्रवाह और अधिक तेज हुआ है और एक अवसर पर 210 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने की शपथ ली। नारायणपुर में भी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने समर्पण किया। यह सम्पूर्ण स्थिति बताती है कि माओवादी हिंसक आंदोलन अब अपनी पकड़ खो रहा है और उसकी ठोस संरचना और मनोबल दोनों चरमरा चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त रणनीति ने इसमें निर्णायक भूमिका निभाई है।
सुरक्षा अभियानों के साथ ही पुनर्वास, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका कार्यक्रमों पर जोर दिया गया, जिससे उन क्षेत्रों में विकास की रोशनी पहुँची जो कभी हिंसा से अंधेरे में डूबे थे। जनजाति युवाओं को शिक्षा और अवसर मिले तो उन्होंने बंदूक छोड़कर नए जीवन की राह चुनी। इस बदलते यथार्थ के बीच एक दूसरी कथा भी गढ़ी जा रही है और वह है वामपंथी नैरेटिव की। यह वही पुरानी शैली है जिसमें शासन को क्रूर बताया जाता है और हिंसा को जन प्रतिरोध कहा जाता है।
सोशल मीडिया और शहरी वामपंथी समूहों द्वारा हिडमा मडावी जैसे कुख्यात माओवादी को “जनजाति योद्धा” के रूप में महिमामंडित करने का प्रयास इसी आखिरी छटपटाहट का हिस्सा है। वामपंथी नैरेटिव का सूत्र हमेशा दो बिंदुओं पर चलता है। पहला शासन को दमनकारी घोषित करना और दूसरा माओवादी हिंसा को स्वाभाविक प्रतिरोध की संज्ञा देना। किसी आतंकवादी की मृत्यु होते ही उसे जंगल का प्रहरी और शोषितों का नायक बना दिया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि माओवादी हिंसा का सबसे बड़ा शिकार स्वयं जनजाति समाज ही है।
वामपंथियों की दूसरी तकनीक है आधा सच बोलकर उसे पूरा नैरेटिव बना देना। सोनी सोरी जैसे मामलों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर पूरी कथा को भावनात्मक दिशा दे दी जाती है जबकि तथ्य, जांच, संदिग्ध कड़ियां और परिस्थितियां कभी सामने नहीं लाई जातीं। सिर्फ भावनात्मक आवरण दिखाया जाता है। इसी रणनीति का उपयोग हिडमा के मामले में भी किया जा रहा है। अब हिडमा मडावी को कुछ समूहों द्वारा जनता का योद्धा बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि वह माओवादी नक्सल संगठन का सबसे हिंसक और क्रूर चेहरा था। उसके नेतृत्व में अनेक जवान मारे गए, जनजाति युवकों को जबरन भर्ती किया गया, महिलाओं का यौन शोषण हुआ, स्कूल और सड़कें उड़ाई गईं और बस्तर के विकास को दशकों पीछे धकेला गया। क्या ऐसे व्यक्ति को जन प्रहरी कहा जा सकता है? वास्तव में यह जनजातियों के नाम पर की जाने वाली सबसे बड़ी धोखाधड़ी है।
इसी के साथ एक और मिथक फैलाया जाता है कि गरीबी नक्सलवाद को जन्म देती है। यदि गरीबी ही कारण होती तो भारत के हर गरीब क्षेत्र में नक्सलवाद होता। भूटान, नेपाल की पर्वतीय जनजातियाँ और भारत के कई अत्यंत गरीब जिले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इससे स्पष्ट है कि नक्सलवाद का असली कारण गरीबी नहीं है, वह तो वैचारिक प्रदूषण, विदेशी समर्थन और शहरों में सक्रिय अर्बन नक्सल नेटवर्क है जो भावनात्मक मुद्दों का उपयोग कर जनजातियों को भ्रमित करता है और उन्हें विकास से दूर रखता है।
जनजाति समाज के अधिकारों, वन संपदा, पंचायत व्यवस्था, शिक्षा और सुरक्षा का वास्तविक संरक्षक भारतीय राज्य ही रहा है। वनाधिकार कानून, पेसा, पंचायत प्रणाली और वन समितियां इन्हीं नीतियों का परिणाम हैं, जिसमें कि माओवादी इन सबको नष्ट करने का प्रयास करते रहे। वे स्कूल और सड़कें उड़ा देते हैं ताकि शिक्षा और प्रशासन वहाँ तक न पहुँच सके। गांवों को भय के वातावरण में रखते हैं और ग्राम सभाओं को बंदूक की नोक पर नियंत्रित करते हैं। इसके बावजूद वामपंथी इन्हें जन प्रतिरोध बताते हैं। यह सत्य से कोसों दूर की कहानी है।
वामपंथियों के दोहरे मापदंड भी किसी से छिपे नहीं। वे उद्योगपतियों पर आरोप लगाते हैं पर स्वयं करोड़ों की संपत्ति में रहते हैं। एनजीओ फंडिंग लेते हैं, विदेश दौरों पर रहते हैं, पर सेवा परियोजनाओं से उनका कोई संबंध नहीं होता। जिन राज्यों में उन्हें लम्बे समय तक शासन चलाने का अवसर मिला वहां गरीबी, हिंसा और अविकास की स्थिति और अधिक गंभीर रही। जबकि सच यही है कि समाधान का मार्ग हिंसा से नहीं, सहभागिता से निकलता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन में स्पष्ट कहा गया है कि समाज की प्रगति समरसता और सहयोग से होती है न कि संघर्ष और हिंसा से। जनजातियों का कल्याण विकास, शिक्षा और स्वावलंबन से ही संभव है न कि माओवादी बंदूक से।
आज जब छत्तीसगढ़ के बस्तर, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में माओवादी प्रभाव तेजी से घट रहा है तो वामपंथी नैरेटिव अपनी अंतिम कोशिश कर रहा है। वे आतंकियों को नायक बनाकर और शासन को क्रूर बताकर पुरानी भावनात्मक पटकथाओं को पुनर्जीवित करना चाहते हैं पर अब यह कोशिश कारगर नहीं रही। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पर्यावरण, मानवाधिकार या क्लाइमेट जस्टिस जैसे सुनने में सार्वभौमिक मुद्दों के नाम पर आंदोलन खड़े किए जाते हैं। किंतु यहां अनेक बार देखा गया है कि इन प्रदर्शनों में अर्बन नक्सल और वैचारिक समूह अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। वे सामान्य और सकारात्मक मुद्दों के भीतर अपना राजनीतिक बीज रोपते हैं। नारे धीरे-धीरे बदलते हैं और पर्यावरण से आगे बढ़कर राज्य विरोध और व्यवस्था विरोध की दिशा में चले जाते हैं।
पर्यावरण इन आयोजनों के लिए केवल बहाना बन जाता है, जबकि लक्ष्य वैचारिक विस्तार और राजनीतिक अस्थिरता की जमीन तैयार करना होता है। यही वह दीमक है जो वर्षों से भारतीय समाज की दरारों में घुसने की कोशिश करती रही है और अब जब नक्सलवाद कमजोर हो चुका है तो यह वैचारिक दीमक अपनी अंतिम चीख पुकार कर रही है।
ऐसे में कहा यही जा सकता है कि माओवादी हिंसा का अंत जरूरी है, यह किसी सरकार या उनसे लोहा ले रहे सुरक्षा बलों की जीत से कहीं अधिक जनजाति समाज की ही जीत है और लोकतंत्र तथा मानवता की भी विजय है। सड़कें बन रही हैं, शिक्षा पहुँच रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं और संवाद मजबूत हो रहा है, यही नक्सलवाद और हिंसक माओवादी आन्दोलन के अंत की सफलता है। यह हम सभी के लिए आनन्द का विषय है कि आज जनजाति समाज अब अराजकता नहीं बल्कि सम्मान, स्थिरता और भविष्य की राह चुन रहा है। यही सच्चा विमर्श है और यही आज के बस्तर तथा भारत का वास्तविक सत्य है। जिसके साथ हर भारतीय को आज पूरे मनोयोग के साथ खड़े होने की आवश्यकता है।
(लेखक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्यक्षेत्र प्रचार प्रमुख हैं।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी