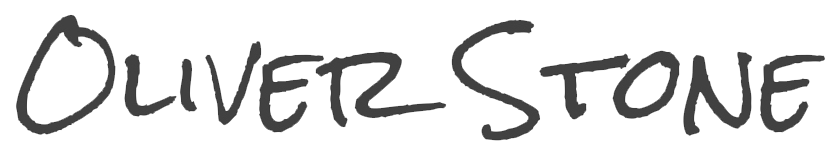Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

हृदयनारायण दीक्षित
ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। गीता की घोषणा है-नहि ज्ञानेन पवित्रमिह विद्यते। ऋग्वेद में ‘ज्ञान’ विषयक एक सूक्त (ऋ0 10.71) है। ‘ज्ञान’ यहां एक देवता हैं। ऋग्वेद के देवता अभिभूत करते हैं। यहां पशु-पक्षी भी देवता हैं। कृषि भी देवता है। साहस (मन्यु) भी देवता हैं। श्रद्धा और हाथ भी देवता है। जहां-जहां दिव्यता वहां-वहां देवता। वस्तुओं मनोभावों को देवता मानने की वैदिक शैली अनूठी है। यही परम्परा ट्रक चालक भी निभाते हैं। वह गाड़ी पर बैठते ही स्टीयरिंग को प्रणाम करता है, सिर झुकाता है चल देता है। लोग ऐसे कृत्यों पर हंसते हैं। हंसना जायज है। स्टियरिंग को प्रणाम करने का कोई तुक नहीं। लेकिन ऋग्वेद में ‘नमस्कार’ भी देवता हैं। मूर्ति, स्टीयरिंग, किताब, पेड़ या नदी को किए गए नमस्कार का सीधा सम्बंध हमारी अंतश्चेतना से है। मूर्ति या स्टीयरिंग नमस्कार के भूखे नहीं है। वे इसका जवाब भी नहीं देते। लेकिन नमस्कार से हमारे मन और काया में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। नमस्कार अंतःकरण को प्रीतिभाव से भरता है।
सृष्टि के प्रारम्भ में कोई एक आदि तत्व या मूलभूत द्रव्य रहा होगा। उसी से भिन्न भिन्न पदार्थो का विकास हुआ। परम तत्व एक से अनेक रूपों में हो गया। ऋषि बताते हैं “अग्रं यत्प्रैरत नामधैयं दधानाः-प्रारम्भिक स्थिति में विभिन्न पदार्थो का नामकरण ही ज्ञान का प्रथम सोपान बना। इनका शुद्ध ज्ञान अनुभूति में होता है और वह अंतः प्रेरणा से प्रकट होता है।” (ऋ0 10.71.1) रूप देखकर नाम रखना, रूप के साथ नाम मिलाकर जानना ज्ञान की शुरूवात है। रूपों के भीतर छुपे गुण-धर्म का ज्ञान अनुभव से ही आता है। यहां अनुभव पर जोर है। जलती अग्नि या बहती हुई नदी दिखाई पड़ीं यह रूप था। नाम रखा गया अग्नि या नदी। रूप के साथ नाम याद रखना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है।
नाम पदार्थ नहीं है। वह वस्तु या पदार्थ का भाषिक प्रतिनिधि है। नाम और रूप मिलाकर ज्ञान बनते हैं। इसके सामाजिक बोध और ज्ञान को साझी बनाने के लिए भाषा चाहिए। भाषा सुबोध चाहिए। सुसंस्कृत भी चाहिए। ऋषि कहते हैं, “सूप से सत्तू स्वच्छ करने की तरह मेधावी जन भाषा गढ़ते हैं और मित्रगण आत्मीय भाव से समझ लेते हैं। ऐसे सफल विद्वान की वाणी में लक्ष्मी का निवास होता है” (वही, मन्त्र 2) भाषा ज्ञानी की वाणी में सरस्वती नहीं लक्ष्मी के निवास का रूपक है। वाणी स्वयं देवी है। वह स्वयं सरस्वती है। भाषा का ज्ञान अतिरिक्त समृद्धि है। इसलिए यहां लक्ष्मी का रूपक है। आगे कहते हैं “ज्ञानियों ने तत्वज्ञानियों के अंतःकरण में प्रविष्ट भाषा को प्राप्त किया। उसे प्रसारित किया।” (वही, मन्त्र-3) ज्ञानी को तत्वज्ञानियों से भाषा संस्कार मिले। तब उनका प्रसार हुआ।
माना जाता है कि जो प्रत्यक्ष है, वह सत्य है, वही ज्ञान है। ऋषि सतर्क करते हैं “अनेक लोग देखकर भी ज्ञान नहीं पाते। अनेक लोग सुनकर भी ज्ञान नहीं पाते। लेकिन सुपात्र के सामने वाणी स्वयं ही अपना सत्य रूप प्रकट कर देती है।” (वही, मन्त्र 4) पढ़कर लिख देना एक शैली है। लोग ऐसे लेखकों को विद्वान कहते हैं। सुना-सुनाया दोहरा देने वाले भी ज्ञानी जैसी प्रतिष्ठा पाते हैं लेकिन ऋषि कहते हैं, “शाब्दिक भावों को ग्रहण करने और उन्हें दोबारा प्रकट करने वाले प्रशंसा पाते है परन्तु उनमें से भी बहुत ऐसे हैं जो भाषा का फल (अर्थ) और फूल (अभिप्राय) नहीं जानते, ऐसे लोग दूध रहित गाय दुहते हैं। वाणी के जरिए प्रपंच करते हैं।” (वही मन्त्र 5) खास बात है अनुभव। अनुभूति ही ज्ञान को वास्तविक बताती है। ऋषि ‘ज्ञान से मित्रता; को जरूरी बताते है “जो सत्य ज्ञान की धारा से मित्रता त्याग देते हैं यस्ति त्याज सचिविदं सखायं-ज्ञान से सखा भाव नहीं रखते, उन्हें दिव्यवाणी (ज्ञान) में अपना हिस्सा नहीं मिलता।” (वही-मन्त्र 6)
ऋग्वेद में एक समान ज्ञानी, एक समान श्रोत्रशक्ति सम्पन्न मेधावी भी ‘एक समान’ नहीं बताये गये। कहते हैं “दर्शन शक्ति सम्पन्न, श्रोत्रशक्ति सम्पन्न, एक समान ज्ञान से युक्त मित्र भी अनुभव जन्य ज्ञान में एक समान नहीं होते।” (वही मन्त्र 7) साथ साथ रहने वाले, आपस में मित्र, एक ही विषय में एक जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान भी अनुभव भिन्नता के कारण एक समान नहीं हो सकते। सत्यबोध ही ज्ञान है। हम सबका इन्द्रिय बोध एक ही पदार्थ के रूप को भिन्न-भिन्न रूप में ग्रहण करता है। सत्य सदा सत्य है। सत्य ‘त्रिकाल अबाधित’ होता है। भूत, भविष्य और वर्तमान उस पर प्रभाव नहीं डालते। अस्तित्व सत्य है। व्यक्त भी सत्य है पर समूचा व्यक्त भिन्न-भिन्न रूपों में विभाजित जान पड़ता है। रूप प्रत्यक्ष हैं, सत्य हैं। परिवर्तनशीलता भी सत्य है। रूप का अंतस्-अव्यक्त सत्य है। अव्यक्त अरूप सदा एक है।
भाषा की शक्ति बड़ी है लेकिन असीम और अनंत नहीं हैं। वस्तु, व्यक्ति या रूप का नाम लेना आसान है लेकिन चित्त में उभरने वाले भावों का वर्णन दुष्कर। परम चेतना विराट है। असीम है। परम चेतन की व्याख्या नहीं हो पाती। भाषा और शब्दों की सीमा है। तब उसकी चर्चा हो कैसे? वैदिक काव्य में परस्पर विरोधी गुणों को जोड़कर विराट को समझाने का रम्य प्रयास है। ‘उसे’ भाषा में समझाया नहीं जा सकता। वह अनुभूति अनिर्वचनीय है, अव्याख्येय है। उसकी व्याख्या असंभव है। पुराणों में उसे अव्याख्येय बताते हुए बड़े दिलचस्प प्रतीक गढ़े गये कि समुद्र को स्याही और हिमालय को कलम बनाकर भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। बड़े से बड़े द्रष्टा, कवि और देवता, आदि भी उसके सामथ्र्य का वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन ऋषियों ने उसे अनुभूति में जाना था। वे गद्गद् थे। परम उल्लास में थे। उल्लास से ही मंत्र काव्य फूटे, लेकिन विराट का वर्णन असंभव था।
विराट को समझना बड़ा कठिन है। प्रगाढ़ अनुभूति में उसका बोध हो भी जाए तो बोध को बताना और भी कठिन। पुराणों में ‘गूंगे के स्वाद’ का प्रतीक इस्तेमाल हुआ है। स्वाद की मधुमयता का बखान गूंगा करे तो कैसे करे? अस्तित्व की अनुभूति का बखान और भी असंभव है।
तुलसीदास ने गाया है “एक दारूगत देखिय एकू/पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू-एक अग्नि प्रत्यक्ष है, वही अग्नि गुप्त है, ब्रह्म भी ऐसा ही है, जो प्रत्यक्ष है वह ब्रह्म, जो अप्रत्यक्ष है वह भी ब्रह्म। ‘व्यक्त’ प्रत्यक्ष हैं, अव्यक्त में वे एक है। ऋग्वेद (10.5.7) में कहते हैं, “असच्च सच्च परमें व्योमन-परम व्योम में सत् असत् दोनों हैं।” सच्च/असच्च हमारी आंखे देखती हैं। इसे समझाने के लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ। असल बात परम व्योम है। मंत्रों के लिए कहते है “ऋचा अक्षर परम व्योमन-ऋचाएं/मंत्र परम व्योम में रहते है।” अव्यक्त परब्रह्म जब व्यक्त प्रकट बनता है तब सत् असत्। सृष्टि का व्यक्त भाग ही इकाई में व्यक्ति है और भाषा में अभिव्यक्ति है। संसार में व्यक्त है अनंत में अव्यक्त और व्यक्त है।
ब्रह्म सम्पूर्णता का पर्यायवाची है। यह वेदांत दर्शन का प्रिय विषय है। ऋग्वेद में प्रकृति की तमाम शक्तियों को विभिन्न देवनाम दिए गये हैं। लेकिन मूल सत्य ‘एकं सद्’ है। उपनिषदों में ऋग्वेद की ‘एकंसद’ (एक ही सत्य) अनुभूति का विकास है। ऋग्वेद में उसे इन्द्र अग्नि और वरूण अदिति जैसे नाम दिए गये। उपनिषदों में उसे ब्रह्म, सच्चिदानंद, प्राण और ईश्वर जैसे अशरीरी/आधिभौतिक नामों से जाना गया। लेकिन नाम से क्या होता है? नाम रूप के साथ ज्ञान से मित्रता जरूरी है।
(लेखक, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश