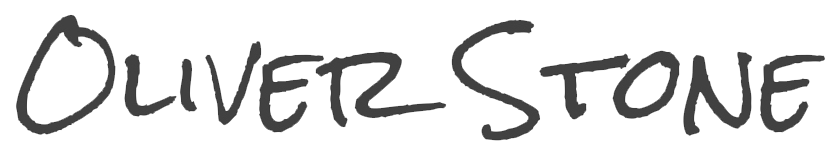Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
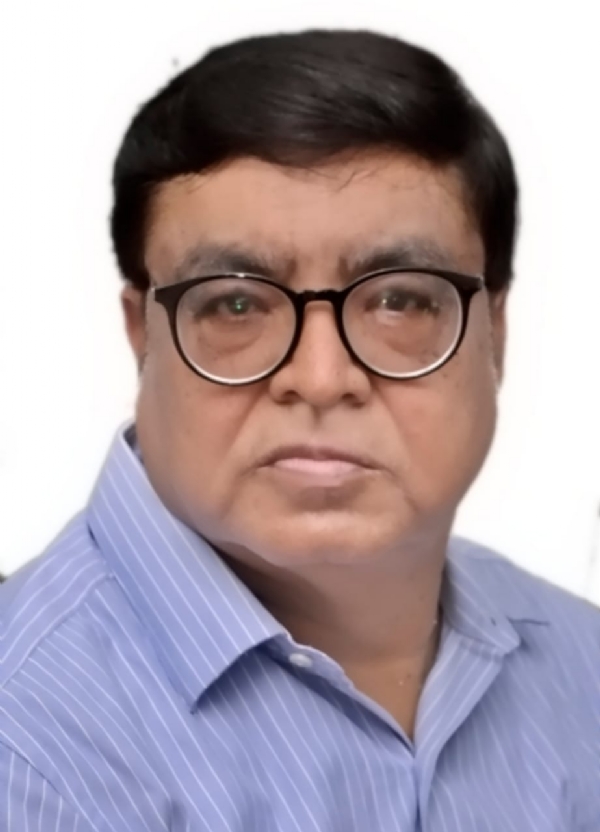
-हरीश शिवनानी
हाल ही भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने जब 16 अक्टूबर को नई दिल्ली में 'यूएन पीसकीपिंग मिनिस्ट्रियल' कॉन्क्लेव में तल्ख़ लहज़े में कहा कि, संयुक्त राष्ट्र आज भी 1945 की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है, न कि 2025 की।” परोक्ष रूप से उनका इशारा पिछले आठ दशकों में यूएनओ की विफलताओं, इसकी संरचनात्मक कमजोरियों और सुधार की आवश्यकता की ओर ही था। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र (यूएनओ) ने अपनी स्थापना के 80 वर्ष पूरे किए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद ‘भावी पीढ़ियों को युद्ध के संकट से बचाने’ के उद्देश्य से स्थापित यह संगठन आज अपनी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता के गंभीर संकट से जूझ रहा है। गाजा, यूक्रेन, सूडान और हैती जैसे वैश्विक संकटों के बीच यूएनओ की निष्क्रियता ने इसे 'कागजी शेर' की संज्ञा दी है।
यूएनओ की विफलताओं का इतिहास खासा लंबा है। यूएनओ की स्थापना का प्राथमिक लक्ष्य विश्व शांति स्थापित करना था लेकिन इसके इतिहास में विफलताओं की लंबी फेहरिस्त है। रवांडा नरसंहार (1994) इसका सबसे दुखद उदाहरण है, जहां यूएन शांति सेना (यूएनएएमआईआर) के रहते हुए भी करीब आठ लाख लोग मारे गए। तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने इसे संगठन की सबसे बड़ी नाकामी माना था। स्रेब्रेनिका नरसंहार (1995) में यूएन द्वारा घोषित सुरक्षित क्षेत्र में 8,000 से अधिक लोगों की हत्या हुई, जिसे रोका नहीं जा सका। इराक युद्ध (2003) में अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप लाखों नागरिक मारे गए। सीरिया गृहयुद्ध (2011 से अब तक) में रूस और चीन के वीटो ने कोई ठोस कार्रवाई रोकी, जिससे 5 लाख से अधिक लोग मारे गए। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण (2022) में भी रूस के वीटो ने यूएन को असहाय बना दिया। हाल के गाजा संकट में अमेरिका ने इजरायल के पक्ष में 53 बार वीटो का उपयोग किया, जिससे युद्धविराम प्रस्ताव विफल हुए। ये घटनाएं यूएन की सबसे बड़ी कमजोरी- सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों (पी-5: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस) के वीटो अधिकार- को उजागर करती हैं।
दरअसल, अपनी स्थापना से ही यूएन कई वैश्विक विवादों को हल करने में असफल रहा है, जो इसकी संरचनात्मक कमियों को दर्शाता है। कुछ उदाहरण देखिए-
स्वेज नहर संकट (1956): यूएन सैन्य समाधान देने में असफल रहा, अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव से ही संकट सुलझा।
कश्मीर विवाद: साल 1948 से प्रस्तावों के बावजूद भारत-पाकिस्तान के बीच यह विवाद यूएनओ कभी सुलझा नहीं पाया। भारत ने अनुच्छेद 370 ख़त्म होने के बाद पीओके को पुनः भारत में विलय का संकल्प दोहराया है।
ईरान-इजरायल संघर्ष: अमेरिका के वीटो के कारण यूएन इजरायल की कार्रवाइयों पर रोक नहीं लगा सका।
फिलिस्तीन-इजरायल संघर्ष: दो-राज्य समाधान लागू नहीं हो सका और इजरायल ने यूएन प्रस्तावों की जमकर अनदेखी की और अंततः गाजा पट्टी को लगभग खत्म ही कर दिया।
सीरिया गृहयुद्ध: रूस और अमेरिका के मतभेदों ने यूएन को बौना साबित कर दिया। इसी तरह उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर यूएन प्रतिबंध प्रभावी नहीं रहे तो पश्चिमी सहारा पर भी जनमत संग्रह कराने में यूएन विफल रहा, साइप्रस विवाद भी दशकों पुराना यह विवाद अनसुलझा है। सबसे बढ़कर पिछले तीन सालों से यूक्रेन-रूस संघर्ष जारी है और हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं पर यूएन बेबस, लाचार बना हुआ है। इन सब वैश्विक घटनाओं को देखते हुए अब यूएन की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि शक्तिशाली देश इसके फैसलों की अवहेलना करते रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। इजरायल ने साल 1967 के युद्ध के बाद कब्जे वाली भूमि से पीछे हटने के यूएन प्रस्तावों को नजरअंदाज किया। अमेरिका ने इजरायल के पक्ष में वीटो का दुरुपयोग किया, जबकि रूस ने यूक्रेन संकट में खुद को बचाया।
भारत की स्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आठ बार अस्थायी सदस्य रहने के बावजूद भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिली। जी-4 देशों (भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान) के साथ मिलकर भारत सुधारों की मांग कर रहा है, लेकिन पी-5 के विरोध ने प्रगति रोकी। निराशा में भारत ब्रिक्स और क्वाड जैसे वैकल्पिक मंचों की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में भारत ने अफ्रीकी प्रतिनिधित्व की वकालत की लेकिन अपनी सदस्यता की अनदेखी से असंतोष बढ़ा है। इसी के मद्देनजर गत 26 सितंबर को महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया और साफ कहा कि “ अब 1945 का दौर नहीं रहा। साल 2024 के 'समिट ऑफ द फ्यूचर' में भी सुधारों पर चर्चा हुई लेकिन पी-5 के बीच तनाव ने रोड़े अटका दिए।
कहने को कहा जा सकता है कि यूएन ने मानवीय सहायता, शरणार्थी संरक्षण और जलवायु पर कुछ सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन इसकी विफलताएं भारी हैं। वीटो पावर, पी-5 का प्रभुत्व और उभरते देशों की अनदेखी ने इसे पक्षपाती बना दिया है। वैकल्पिक मंचों जैसे ब्रिक्स और जी20 का उदय यूएन की प्रासंगिकता को चुनौती दे रहा है। सुधारों के बिना यूएन लीग ऑफ नेशंस की तरह अप्रासंगिक हो सकता है। आवश्यक सुधारों के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं:
वीटो पावर पर अंकुश: सुरक्षा परिषद के पाँच देशों के वीटो के दुरुपयोग को सीमित करना।
स्थायी सदस्यता का विस्तार: भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीकी देशों को शामिल करना अब अपरिहार्य हो चुका है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में इनकी भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। गत 80 वर्षों में यूएन ने विश्व शांति के लिए कुछ प्रयास किए लेकिन रवांडा, स्रेब्रेनिका, इराक, सीरिया, यूक्रेन और गाजा जैसे मामलों में इसकी विफलताएं इसकी विश्वसनीयता पर बट्टा लगाती हैं। यदि यूएन 2025 की दुनिया के अनुरूप खुद को नहीं ढालता तो यह केवल भाषणों का क्लब बनकर रह जाएगा। सुधार ही इसका भविष्य तय करेंगे- वरना अप्रासंगिक बन कर रह जाना ही इसकी नियति होगी।
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश