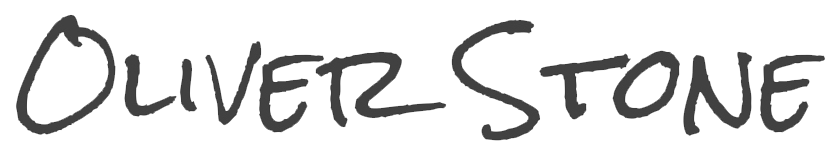Enter your Email Address to subscribe to our newsletters


कैलाश चन्द्र
दिल्ली में साल 2020 के दंगे योजनाबद्ध अराजकता, राजनीतिक संरक्षण और वैचारिक उद्दीपन का भयावह उदाहरण थे। यह हिंसा अचानक भड़की कोई घटना नहीं थी बल्कि इसके पीछे महीनों से तैयार किया गया ऐसा तंत्र था, जिसमें शब्दों को हथियार और भीड़ को औजार बनाया गया। इन दंगों में 53 निर्दोष लोगों की जान गई। इनमें एक होनहार खुफिया अधिकारी अंकित शर्मा, पौड़ी गढ़वाल से दिल्ली रोजगार की तलाश में आया दिलबर नेगी और दो पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इन हत्याओं की क्रूरता ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया, किंतु उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह रही कि पीड़ितों का दर्द धीरे-धीरे हाशिये पर चला गया और आरोपितों के लिए सहानुभूति का एक संगठित नैरेटिव खड़ा किया गया।
अंकित शर्मा, जो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी संस्था के लिए कार्यरत थे, उनके शरीर पर 74 चाकू के घाव मिले। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, एक संदेश था। वहीं दिलबर नेगी, एक गरीब मां का बेटा, जिसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी, उसके हाथ-पैर काट कर उसे जिंदा जला दिया गया। सवाल यह है कि क्या यह केवल दंगा था या फिर भीड़ की हिंसा को वैचारिक समर्थन देने वाली मानसिकता का परिणाम?
इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक विचलित करने वाला पक्ष यह है कि जिन लोगों पर इस हिंसा की साजिश रचने और उसे भड़काने के गंभीर आरोप हैं, उनके बचाव में खड़े होने वाले वकील कोई साधारण नाम नहीं हैं। ये सभी देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे आरोपितों की पैरवी करने वालों में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, अश्विनी कुमार जैसे नाम शामिल हैं, जो देश में कांग्रेस सरकारों के समय बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। इनके साथ सिद्धार्थ दवे, सिद्धार्थ लूथरा और त्रिदीप पैइस जैसे वरिष्ठ वकील भी जुड़े रहे। ऐसे में ये सिर्फ कानूनी सहायता का मामला नहीं लगता, साफ तौर पर एक विशेष वैचारिक झुकाव का संकेत देता है।
यहां प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस और उससे जुड़े वैचारिक तंत्र को पीड़ितों की चीखें सुनाई नहीं देतीं। क्या अंकित शर्मा की मां का विलाप उन्हें विचलित नहीं करता। लेकिन वही तंत्र उमर खालिद और शरजील इमाम में लोकतंत्र का रक्षक और अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक खोज लेता है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि सोची-समझी विचारधारा का परिचय है, जहां राष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियों को संदेह के घेरे में रखा जाता है और दंगों के आरोपित नैरेटिव के नायक बना दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कांग्रेस को पीड़ितों की चीखें नहीं दिखतीं, पर आरोपितों में वह पीड़ित ढूँढ लेती है। वह अंकित शर्मा जैसे शहीद अधिकारी की निर्मम हत्या को राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं बनाती, पर “टुकड़े-टुकड़े गैंग” के पोस्टरबॉय को लोकतांत्रिक अधिकारों की कथा बनाकर प्रस्तुत करती है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक विचारधारा का परिचय है, जहाँ राष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियाँ गलत और दंगों के आरोपी “नैरेटिव हीरो” बन जाते हैं। यही वह नैरेटिव-निर्माण है जिसने देश को भ्रमित किया, जहाँ अपराधी को एक्टिविस्ट और पीड़ित को अदृश्य कर दिया जाता है। जमानत दंगे के हत्यारों का अधिकार कैसे..? सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल कानूनी सहायता है या किसी विशेष मानसिकता का स्पष्ट संकेत?
सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय इस पूरे विमर्श में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर है और दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय हैं। अदालत ने यह भी कहा कि इस प्रकार की संगठित और हिंसक साजिश में शामिल लोगों को इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि वे लंबे समय से जेल में हैं। इसे समझें तो यह टिप्पणी नैतिक संदेश भी है कि कानून भावनाओं या राजनीतिक दबाव से संचालित नहीं होगा। हालांकि अदालत ने कुछ अन्य आरोपितों को सख्त शर्तों के साथ जमानत दी, पर साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि शर्तों के उल्लंघन पर उन्हें दोबारा जेल भेजा जा सकता है। इससे यह संदेश गया कि न्यायपालिका ने साजिश और हिंसा की गंभीरता को केंद्र में रखकर निर्णय दिया है, न कि किसी नैरेटिव या जनमत के दबाव में।
जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि यह हिंसा अचानक नहीं भड़की थी। आम आदमी पार्टी का तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन इस हिंसा में एक प्रमुख भूमिका में सामने आया। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और डिजिटल साक्ष्यों से संकेत मिला कि उसकी छत से पेट्रोल बम फेंके गए और दंगाइयों के लिए संसाधन जुटाए गए। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का नाम भी कई बयानों में सामने आया। यह भी एक कड़वा सत्य है कि इस दंगे में सबसे अधिक नुकसान हिंदुओं को हुआ, चाहे वह जान-माल का हो या धार्मिक स्थलों का।
इसके समानांतर एक और चिंताजनक परत सामने आई, मीडिया और तथाकथित इकोसिस्टम पत्रकारिता की। अजित अंजुम और आरफा खानम जैसे नाम उमर खालिद और शरजील इमाम के लिए संवेदना, आक्रोश और पीड़ा व्यक्त करते दिखाई दिए, लेकिन अंकित शर्मा के परिजनों का दर्द उन्हें शायद ही दिखाई दिया। यह वही नैरेटिव निर्माण है, जिसमें अपराधी को एक्टिविस्ट और पीड़ित को अदृश्य कर दिया जाता है। यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि दंगे में शामिल हत्यारों की जमानत को मानवाधिकार का विषय कैसे बना दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर यह कहते हुए निशाना साधा कि यह कांग्रेस इकोसिस्टम पर करारा तमाचा है, तो यह केवल राजनीतिक बयान नहीं था। निश्चित ही यह उस नैरेटिव की हार थी, जो वर्षों से गढ़ा जा रहा था। अदालत के निर्णय ने उन तमाम लेखों, बहसों और अभियानों को अप्रासंगिक कर दिया जिनका उद्देश्य आरोपितों को मासूम और पीड़ितों को संदिग्ध साबित करना था।
दिल्ली के साल 2020 के दंगे केवल एक शहर की त्रासदी नहीं थे, यह भारत के लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और मीडिया की भूमिका की भी परीक्षा थे। इतिहास केवल अदालतों में नहीं लिखा जाता, वह जनता की स्मृति में भी अंकित होता है। अंकित शर्मा और दिलबर नेगी की पीड़ा उस स्मृति का हिस्सा है। इतिहास न्याय करता है और जनता भी आखिरकार न्याय ही चाहती है, हम ये नहीं भूलें। इस पूरे प्रकरण का सार यही है जो दल, नेता, पत्रकार और बुद्धिजीवी दंगाइयों के साथ खड़े होंगे, जनता उन्हें कितने भी प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय, देशभक्तपूर्ण नहीं मान सकती। जो तंत्र शहीदों को भुलाकर आरोपितों को निर्दोष साबित करने में अपनी ऊर्जा लगाए, उसकी नीयत और राष्ट्रभक्ति दोनों कटघरे में खड़ी होती है।
(लेखक, वरिष्ठ स्तंभकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं।)
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी