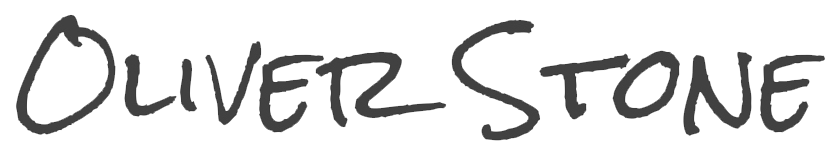Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

-डॉ सत्यवान सौरभ
जाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में बच्चों के अधिकारों और सामाजिक पहचान की उपेक्षा गंभीर चिंता का विषय है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि यदि कोई बच्चा अनुसूचित जाति की मां द्वारा पाला गया है और उसी समुदाय के रीति-रिवाजों में बड़ा हुआ है, तो उसे प्रमाणपत्र से वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही पिता की जाति भिन्न हो। यह फैसला बच्चों के संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब आवश्यक है कि राज्य सरकारें स्पष्ट नीति बनाकर प्रशासनिक भेदभाव की समाप्ति सुनिश्चित करें।
जाति प्रमाणपत्र एक ऐसा दस्तावेज है, जो हमारे समाज की सामाजिक संरचना और संवैधानिक वादों के बीच की गहरी खाई को उजागर करता है। यह केवल आरक्षण या सरकारी योजनाओं की पात्रता का प्रमाण नहीं, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि किसी बच्चे को अपने अधिकार पाने के लिए किस प्रकार की सामाजिक स्वीकृति और सरकारी मान्यता की आवश्यकता है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति से संबंधित किसी व्यक्ति का बच्चा भी उसी जाति से माना जाएगा, भले ही उसके माता-पिता के बीच धर्म अलग-अलग हों। यह फैसला उन हजारों बच्चों को राहत देता है, जिन्हें आज भी केवल उनके माता-पिता के धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर जाति प्रमाणपत्र से वंचित किया जा रहा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला एक बहुचर्चित मामले में आया, जिसमें एक विधवा महिला ने अपने बेटे के लिए अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र की मांग की थी। महिला दलित समुदाय से थी, जबकि उसके पति अन्य धर्म से संबंधित थे। बच्चे का पालन-पोषण दलित परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक परिवेश में हुआ, लेकिन प्रशासन ने प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर दिया। तर्क था – पिता की जाति अलग थी, अतः बच्चा उस जाति का नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह दृष्टिकोण न केवल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों के विकास के अवसरों पर भी आघात है।
न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि “जाति एक सामाजिक निर्माण है, जैविक नहीं। यदि बच्चा उस जाति के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में बड़ा हुआ है, तो उसे उस समुदाय का हिस्सा माना जाना चाहिए।” यह टिप्पणी उन सरकारी अधिकारियों के सोच पर गहरी चोट है, जो जाति को अब भी 'खून से बंधा हुआ' तत्व मानते हैं, न कि सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 समानता का अधिकार प्रदान करता है, वहीं अनुच्छेद 46 स्पष्ट रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सुरक्षा की बात करता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। सरकारी दफ्तरों में आज भी जाति प्रमाणपत्र एक 'कागजी पहचान' से ज़्यादा एक 'पैदाइशी सबूत' के रूप में देखा जाता है। अधिकारी, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऐसे दस्तावेज़ माँगते हैं जो एक साधारण नागरिक के पास हों भी तो उन्हें मान्यता नहीं मिलती — जैसे मौखिक घोषणाएं, स्थानीय पंचायत की सिफारिश, या जातिगत मान्यता पत्र।
समस्या की जड़ उस मानसिकता में है, जो मानती है कि जाति पिता से तय होती है, न कि सामाजिक पालन-पोषण और सामाजिक पहचान से। विशेषकर जब माता अनुसूचित जाति की हो और पिता अन्य जाति या धर्म का, तो बच्चे की पहचान को लेकर सरकारी तंत्र असहज हो जाता है। बच्चों को उन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, जिनके वे जन्मसिद्ध हकदार हैं — केवल इसलिए कि वे ‘शुद्ध जाति व्यवस्था’ के साँचे में फिट नहीं होते।
यहाँ एक और प्रश्न उठता है- क्या जाति प्रमाणपत्र के मामले में 'पालन-पोषण' का महत्व नहीं होना चाहिए? क्या एक बच्चा जो दलित बस्ती में पला-बढ़ा, जिसने सामाजिक अपमान, भेदभाव और आर्थिक अभाव झेला, उसे केवल इस आधार पर वंचित किया जा सकता है कि उसके पिता किसी अन्य जाति या धर्म से थे? दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया — कि जाति कोई आनुवंशिक रोग नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तराधिकार है।
प्रशासनिक व्यवस्था आज भी औपनिवेशिक सोच से ग्रस्त है, जहाँ हर दस्तावेज़ को संदेह की निगाह से देखा जाता है। बच्चे और विधवा महिलाओं के मामलों में तो यह और भी जटिल हो जाता है। एक विधवा दलित महिला को बार-बार प्रमाण देना पड़ता है कि उसका बच्चा उसी समुदाय में बड़ा हुआ है — यह न केवल मानसिक पीड़ा है, बल्कि असंवेदनशील राज्य व्यवस्था का प्रत्यक्ष उदाहरण भी है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) भी कई बार यह सुझाव दे चुका है कि बच्चों को जाति प्रमाणपत्र जारी करने में ‘पालन-पोषण’ को एक प्रमुख आधार बनाया जाए। लेकिन राज्य स्तर पर नौकरशाही अभी भी इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। अधिकारियों को डर है कि यदि सामाजिक पहचान को आधार मान लिया गया, तो फर्जी प्रमाणपत्रों की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन यह सोच असल में उन बच्चों के अधिकारों का हनन करती है, जो दोहरे भेदभाव का शिकार होते हैं — एक ओर सामाजिक, दूसरी ओर प्रशासनिक।
जाति प्रमाणपत्र न केवल आरक्षण की कुंजी है, बल्कि यह सरकारी छात्रवृत्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, आवासीय योजनाओं और नौकरियों में प्रवेश का द्वार भी है। जब किसी बच्चे को केवल उसके माता-पिता की जातिगत भिन्नता के आधार पर इससे वंचित किया जाता है, तो यह संविधान की आत्मा पर आघात है। यह उस समानता और न्याय की भावना के विपरीत है, जिसकी स्थापना के लिए संविधान निर्माताओं ने संघर्ष किया था।
यह भी उल्लेखनीय है कि कई बार तो अधिकारियों द्वारा जाति प्रमाणपत्र देने से इनकार करने के पीछे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या राजनैतिक दबाव भी होता है। यदि कोई बच्चा गरीब है, दलित बस्ती में रहता है और उसकी माँ अकेली कमाने वाली है- तब भी उसे प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता, जब तक वह ‘पिता की जाति’ सिद्ध न कर दे। यह पुरुषसत्तात्मक दृष्टिकोण है, जो महिला की सामाजिक स्थिति और उसके बच्चे के अधिकारों को नगण्य समझता है।
ऐसे में न्यायालयों की भूमिका निर्णायक हो जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला एक नज़ीर बने, इसके लिए ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारें स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें। यदि कोई बच्चा किसी दलित महिला द्वारा पाला गया है, और समाज में उसकी पहचान उस समुदाय की है, तो उसे जाति प्रमाणपत्र देने में कोई संदेह या अड़चन नहीं होनी चाहिए। साथ ही, बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में भी यह आवश्यक है कि शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और बाल आयोग मिलकर ऐसी नीतियाँ बनाएँ, जहाँ बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि को वरीयता दी जाए- न कि केवल जैविक वंशावली को।
यह केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि संवैधानिक न्याय की ओर एक कदम है। यदि हम बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित करेंगे, तो वह राष्ट्र जो ‘न्याय, स्वतंत्रता और समानता’ की बात करता है, केवल एक छलावा बनकर रह जाएगा।
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश