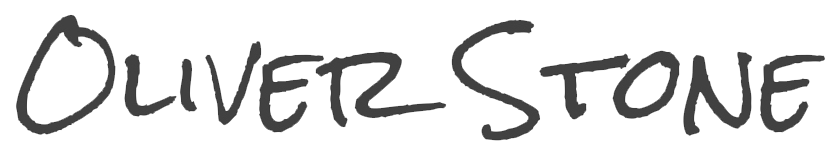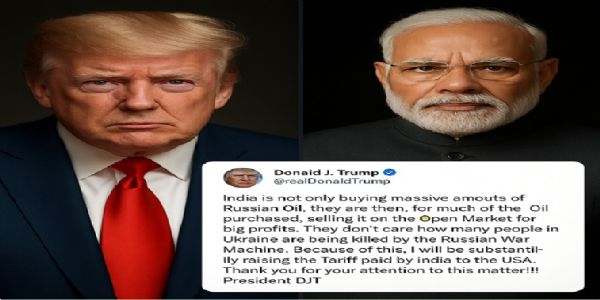Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

अक्षय ऊर्जा दिवस (20 अगस्त) पर विशेष
- योगेश कुमार गोयल
पृथ्वी पर ऊर्जा के परम्परागत साधन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसे में खतरा मंडरा रहा है कि यदि ऊर्जा के इन पारम्परिक स्रोतों का इसी प्रकार दोहन किया जाता रहा तो इन परम्परागत स्रोतों के समाप्त होने पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही कारण है कि पूरी दुनिया में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जाने लगी और इसी कारण अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करने के प्रयास शुरू हुए। अक्षय का अर्थ है, जिसका कभी क्षय न हो अर्थात् अक्षय ऊर्जा वास्तव में ऊर्जा का असीम और अनंत विकल्प है और आज के समय में यह किसी भी राष्ट्र के अक्षय विकास का प्रमुख स्तंभ भी है। पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए ऐसी ऊर्जा तथा तकनीकें विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग की विकराल होती समस्या से दुनिया को कुछ राहत मिल सके। किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए आज प्रदूषणरहित अक्षय ऊर्जा स्रोतों का समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता भी है। देश में अक्षय ऊर्जा के विकास और उपयोग को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए ही वर्ष 2004 से हर साल 20 अगस्त को ‘अक्षय ऊर्जा दिवस’ भी मनाया जाता है।
आज न केवल भारत में बल्कि समूची दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। ऐसे में अक्षय ऊर्जा ही ऐसा विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ-साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी कारगर साबित होगी लेकिन अक्षय ऊर्जा की राह में भी कई चुनौतियां मुंह बाये सामने खड़ी हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन की देशभर में कई छोटी-छोटी इकाईयां हैं, जिन्हें एक ग्रिड में लाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इससे बिजली की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भारत में अक्षय ऊर्जा के विविध स्रोतों का अपार भंडार मौजूद है लेकिन इनसे ऊर्जा उत्पादन करने वाले अधिकांश उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार, कुछ साल पहले सौर ऊर्जा के लिए करीब 90 प्रतिशत उपकरण विदेशों से आयात किए गए थे, जिससे बिजली उत्पादन की लागत काफी बढ़ गई। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, अब भी भारत की सौर सेल और मॉड्यूल की जरूरत का अधिकांश हिस्सा, कभी-कभी 90 प्रतिशत तक, आयात से ही पूरा होता रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में एएलएमएम नियम और पीएलआई स्कीम के कारण यह निर्भरता घट रही है। 2023-24 में चीन से सौर सेल्स का 53 प्रतिशत और मॉड्यूल्स का 63 प्रतिशत भारत में आया।
देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर भी तेजी से बढ़ रहा है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 450 गीगावॉट से अधिक हो चुकी है, जिसमें अब 230 गीगावॉट से अधिक अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो-पावर और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अधिक बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से तथा परमाणु ऊर्जा से भी अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। कुल बिजली उत्पादन में अब अक्षय ऊर्जा का हिस्सा अब लगातार बढ़ रहा है, जो भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करता है।
भारत में ऊर्जा खपत भी तेजी से बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि वर्ष 2040 तक भारत में ऊर्जा की कुल मांग वर्तमान की तुलना में लगभग दोगुनी हो जाएगी। विशेषकर बिजली तथा ईंधन के रूप में उपभोग की जा रही ऊर्जा की मांग घरेलू एवं कृषि क्षेत्र के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में ही बिजली तथा पैट्रोलियम जैसे ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों का लगभग 55 प्रतिशत उपभोग किया जाता है। हम जिस बिजली से अपने घरों, दुकानों या दफ्तरों को रोशन करते हैं, जिस बिजली या पैट्रोलियम इत्यादि ऊर्जा के अन्य स्रोतों का इस्तेमाल कर खेती-बाड़ी या उद्योग-धंधों के जरिये देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया जाता है, क्या हमने कभी सोचा है कि वह बिजली या ऊर्जा के अन्य स्रोत हमें कितनी बड़ी कीमत पर हासिल होते हैं? यह कीमत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी धरती पर विद्यमान हर प्राणी पर बहुत भारी पड़ती है। भारत में थर्मल पावर स्टेशनों में बिजली पैदा करने के लिए प्रतिदिन लगभग 18 लाख टन कोयले की खपत होती है। आज भी देश की लगभग 55 प्रतिशत से अधिक बिजली कोयले से ही पैदा होती है, शेष बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों, जल, गैस व परमाणु ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है।
दुनियाभर में ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन बिजली उत्पादन से ही होता है। यही कारण है कि अब सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, यदि अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाए तो वर्ष 2050 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 70 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। भारत ने भी 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने और नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष 2070 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने से हमारी ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर कम होता जाएगा और इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
भारत में अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्मार्ट ग्रिड, बैटरी स्टोरेज और इलैक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे कदम भी तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जो अक्षय ऊर्जा को व्यावहारिक और टिकाऊ बनाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि निर्यातक देश भी बन सकेगा। सही मायने में अक्षय ऊर्जा ही आज भारत में विभिन्न रूपों में ऊर्जा की जरूरतों का प्रमुख विकल्प है, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ टिकाऊ भी है। भारत धीरे-धीरे ही सही, अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज समय है कि हम आर्थिक बदहाली और भारी पर्यावरणीय विनाश की कीमत पर ताप, जल एवं परमाणु ऊर्जा जैसे पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय अपेक्षाकृत बेहद सस्ते और कार्बन रहित पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोतों के व्यापक स्तर पर विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ें। साथ ही हमें ऊर्जा की बचत की आदतें भी अपनानी होंगी क्योंकि ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग ही हमें सुरक्षित, समृद्ध और स्वच्छ भविष्य की ओर ले जाएगा।
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश