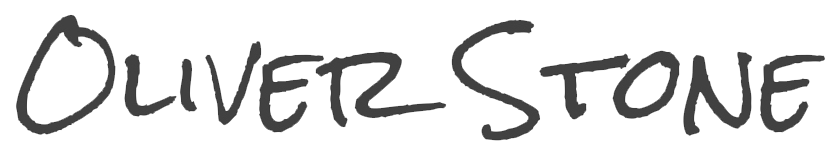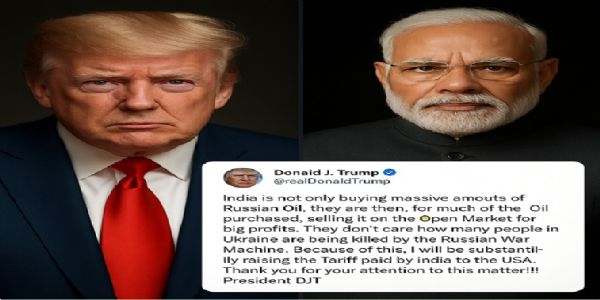Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल
भारतीय जीवन-पद्धति में गुरु का अप्रतिम स्थान है। ज्ञान को सर्वोकृष्ट माननेवाली इस परंपरा में गुरु के बिना कुछ भी लभ्य नहीं है। शायद दुनिया में भारत एकमात्र देश है, जिसकी परंपरा, इतिहास और संस्कृति में चाहे जितना परिवर्तन आया हो, गुरु के स्थान एवं उसकी मान्यता में कोई विचलन नहीं दिखाई देता। यद्यपि यह भी सच है कि आधुनिक युग में स्वयं गुरु के स्वरूप एवं उसकी क्रियात्मकता में अंतर आया है, किंतु समाज में विविध प्रकार के आदर्शों की च्युति के बाद भी गुरु का स्थान अद्वितीय है। भारत के प्राचीनतम ज्ञात इतिहास से विचार कर, गुरु या आचार्य को देवता माना गया है। स्मृतियों में तो गुरु को पिता से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि गुरु ऐसे जीव को, जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि पाशविक प्रवृत्तियों के चलते पशु से भिन्न नहीं है, को ज्ञान के आलोक से प्रकाशित कर धर्म-मूल्य से समन्वित कर मनुष्य बनाता है।
भारत की सनातन धारा में स्पष्टतः परिलक्षित होनेवाली आगमिक और निगमिक दोनों परंपराएँ गुरु-केंद्रित हैं। यह भी कहा जा सकता है, गुरु तत्त्व का ज्ञान भारत का ज्ञान है और आगम परंपरा में गुरु का महत्त्व ही नहीं है, अपितु इस धारा के समस्त ग्रंथ गुरु-महिमा और उसके स्वरूप का अत्यंत विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते हैं। निगम की परंपरा में जहां गुरु एक बार सत्य का दर्शन कराकर शिष्य को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। वहीं आगमिक परंपरा में जीवन की अविकसित स्थिति से ऊपर उठाते हुए आत्म-विकास और पूर्णता को प्राप्त करने के लिए निरंतर पथ-प्रदर्शक और सहायक की आवश्यकता होती है। आगम का यह मार्ग अनुभवसिद्ध एवं तर्कसिद्ध है, क्योंकि जगत के पदार्थों अर्थात् भौतिक विषयों एवं भौतिक पद संबंधों का ज्ञान भी गुरु की अपेक्षा करता है। जिसे भूल और प्रयत्न विधि से भी सीखा जा सकता है। जिस व्यवहार को पशु सहज प्रवृत्ति से ही प्राप्त कर लेते हैं, उसे भी सीखने के लिए मनुष्य को गुरु की आवश्यकता होती है, तो अपूर्णताओं को अतिक्रांत कर, उनका विलोप कर, आत्मपूर्णता की स्थिति बिना गुरु के कैसे प्राप्त होगी ?
स्वरूपतः मनुष्य जो है, उसकी उसे स्मृति नहीं होती अविद्याजन्य संस्कारों के कारण वह आत्मविस्मृति का शिकार रहता है। अविद्या के नाश और विद्या के प्रकाशमय जगत् में प्रवेश के लिए गुरु आवश्यक है। वह पाशविक अनुभव के धरातल से चैतसिक अनुभूति के स्तर तक समुन्नत करने का साधन है। आगमसार ग्रंथ में गुरु के इस स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि गुरु शब्द का 'गकार' सिद्ध देनेवाला, 'रकार' पाप का दहन करनेवाला है और 'उकार' स्वयं शंभू है, अर्थात् ज्ञान और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाले पापों का नाश गुरु ही करता है। वह मात्र नाश ही नहीं करता, बल्कि भौतिक एवं आध्यात्मिक सिद्धियों का प्रदाता भी है। यह सभी नहीं कर सकते, अतः गुरु होने की योग्यता भी है, शर्तें भी। 'नवचक्रेश्वरतंत्र' में कहा गया है कि पिंड, पद, रूप और रूपातीत; इस सबको जो सम्यक् ढंग से जानता है, वही गुरु कहा जाता है, अर्थात् मात्र भौतिक या केवल आध्यात्मिक ज्ञानवाला गुरु नहीं हो सकता। गुरु होने के लिए आवश्यक है कि वह इन सबको जानता हो, न केवल जानता हो अपितु सम्यक् रूप से जानता हो। रुद्रयामल, मुंडमाला इत्यादि ग्रंथों में गुरु, मंत्र और देवता इन तीनों को एकाकार बताया गया है, मुंडमालातंत्र में तो गुरु को देवताओंके पितामह के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है।
गुरु का महत्त्व भारतीय परंपरा में मात्र तांत्रिक और वैदिक साधना तक सीमित नहीं रहा है, अपितु संत परंपरा में भी इसका पर्याप्त महत्त्व है। कबीरदास की बानी तो जन-जन जानता है कि 'बलिहारि गुरु आपनो गोविंद दियो बताय'। काशी के ही अघोर संत बाबा किनाराम ने गुरु की महिमा बताते हुए कहा कि गुरु चारों वेद हैं, वहीं अग्नि, पवन, जल, धरती, आकाश इत्यादि पंचमहाभूत भी हैं, अर्थात् गुरु सभी का मूल हैं, सभी प्रकार के शूलों का हरण करनेवाला है। यह नित्य, अमल और अपने शिष्य को पावन पद को देनेवाला है।
यह गुरु ही है, जो गोविंद तक पहुंचाता है, इसलिए वह आध्यात्मिक अभ्युदय का साधन है। ज्ञान के उदय के साथ गुरु ही गोविंद हो जाता है। सकल संशयों की निवृत्ति उसके प्रति सर्वविध समर्पण से ही संभव है। इसलिए गुरु से किसी प्रकार की वंचना उचित नहीं है। स्कंदपुराण के उत्तर खंड में गुरु-तत्त्व के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जिसके सत्य होने पर ही जगत् की सत्ता है, जिसके प्रकाश से सबकुछ प्रकाशित होता है, जिसके द्वारा आनंद प्राप्त होता है, उस गुरु को प्रणाम है। संक्षेपतः यह कहा जा सकता है कि गुरु-तत्त्व के प्रकाशित होने से ही जगत् प्रकाशित होता है और जागतिक वस्तुओं का ज्ञान तथा जगत् में अभ्युदय की प्राप्ति होती है। साथ ही जगत् की सीमा का अतिक्रमण करवह परम निःश्रेयस की अवाप्ति भी कराता है।
भारतीय परंपराक्रम में अध्यात्म-विद्या की साधना में ही गुरु का महत्त्व नहीं है, अपितु ज्ञान की भौतिक साधना भी गुरु-केंद्रित है। इसलिए आचार्य को देवता कहा गया है। स्मृतिकारों ने अक्षरमात्र प्रदात्त को योनि संबंधों में श्रेष्ठ माने जानेवाले संबंधों से श्रेष्ठकर स्वीकार किया है। मनु ने कहा है कि पिता गार्हपत्याग्नि है, माता दक्षिणाग्नि है तथा गुरु आहवनीयाग्नि है। जिस प्रकार तीनों अग्नियों में आहवनीयाग्नि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार गुरु इन तीनों में श्रेष्ठ है। यह श्रेष्ठता मात्र श्रद्धा पर आधारित नहीं है। इसके लिए शर्तें हैं, जो गुरु इन शर्तों को पूरा करता है, वही श्रद्धा का पात्र है। इसकी चर्चा शारदातंत्र एवं विश्वसारतंत्र में विस्तृत रूप से प्राप्त होती है। सभी शास्त्रों में वर्णित शर्तों को संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया जाए तो कहा जा सकता है कि जो सभी शास्त्रों में दक्ष तथा सर्वशास्त्रार्थविद्, जितेंद्रिय, सत्यवादी, शांत मानस, सर्वकर्मपरायण, गृहस्थ, निरोगी, निरहंकार तथा विकाररहित है, वही गुरु होने के योग्य है।
गुरु के भी शिक्षा तथा दीक्षा दो प्रकार के भेद हैं दीक्षा-गुरु वही हो सकता है, जिसमें सतर्क की प्रतिष्ठा हो गई हो, अर्थात् जिसमें संस्कारित विकल्पों का प्रादुर्भाव हो गया है। सतर्क ही भावना है, भावना का अर्थ है भूत-अभूत सभी अर्थों का स्फुट भावन। यह भावना ही निर्जीव अक्षरों में चेतना को उद्भूत करती है और भौतिक ज्ञान भी चैतसिक हो उठता है, किंतु शिक्षा-गुरु का दायित्व सत्-असत् का विवेक, ग्राह्य-अग्राह्य का भेद ज्ञान कराना मात्र है। तंत्रों में उसे असद् गुरु तथा स्मृतियों में आचार्य कहा गया है। आचार्य वह है जिसे ज्ञान है, यद्यपि उसके साथ उसकी एकाकारिता नहीं है। वह जानता है और बताता भी है, किंतु वहाँ तक पहुँचा नहीं सकता। जगत् की सीमा से परे, पदों एवं संबंधों से ऊपर नहीं ले सकता। परिणामतः वह मन में बंधन को तोड़ने की इच्छा और साहस तो उत्पन कर देता है, तोड नहीं पाता। सबकुछ बताकर वह विद्या-स्नान कराता है और समावर्तन का उपदेश करता है। इस उपदेश के साथ उसे स्नातक घोषित करता है। साथ ही आचरण के पक्ष को लेकर वह सावधान भी करता है कि हमारा जो सुचरित्र है, वही तुम्हारे लिए अनुकरणीय है, अन्य नहीं।
गुरु के महत्व को आज के संदर्भों में भी समझना होगा। दोनों ही प्रकार के गुरु, जिनका शास्त्रीय स्वरूप विवेचित किया गया है, उसकी आज के संदर्भों में परीक्षा करनी होगी, क्योंकि आज जो लोक को ग्राह्य है, स्वीकार्य है, वही धर्म है। शास्त्र शुद्धि होते हुए भी लोक-विरुद्ध होने पर आचरण योग्य नहीं होता। जो लोक की उपेक्षा करता है, वह निंदा का पात्र होता है। अतः आधुनिक शिक्षा- व्यवस्था के संदर्भ में शिक्षा गुरु, अर्थात् आचार्य एवं धर्मोपासना के वर्तमान संदर्भों में विचार करें तो ध्यान में यह रखना आवश्यक है कि परंपरा के क्रम में आचार्य वही है, जो सकल वेदराशि, अर्थात् ज्ञान का संकल्प और सरहस्य अध्यापन करे। एकदेशीय अध्यापक, पण्यजीवी अध्यापक, आचार्य न होकर उपाध्याय है।
यही कारण है कि महाभारत में सांदीपनि विद्या में, प्रताप में न्यून होने के बाद भी द्रोण की अपेक्षा आदरणीय एवं पूज्य हैं सांदीपनि का शिष्य कृष्ण कहीं उनके विरोध में खड़ा नहीं होता। वह गुरु को प्रसन्न करने के लिए मृत्यु के समान भयंकर पांचजन्य से भी युद्ध करता है और कभी संधि नहीं करता, पांचजन्यों के क्षेत्र में ही द्वारिका की स्थापना के बाद भी नहीं। जबकि पण्यजीवी द्रोण के शिष्य गुरु-दक्षिणा देकर उससे मुक्त हो जाते हैं और गुरु के धुर विरोधी द्रुपद से संबंध जोड़ते हैं, उससे मित्रता करते हैं। इसके निहितार्थ को आधुनिक संदर्भों में देखना होगा। वृत्ति के लिए अध्यापन कर्म करनेवाला आचार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह वृत्तिदाता की शर्तों के अधीन है। वह राज्य या ऐसी किसी भी संस्था, जिससे वित्तपोषित है, उसके विरुद्ध सोच भी नहीं सकता। वह हस्तिनापुर के खूंटे से बँधा हुआ द्रोण के समान है, चाहे उस पर पांडु बैठा हो या दृष्टि और विवेक दोनों से विहीन धृतराष्ट्र, जिनकी दासता को स्वीकार करना है। उसे सत् के पक्ष में खड़े होने का साहस नहीं होता। वह स्वयं भी उस दुर्योधन से अलग मनःस्थिति में नहीं होता, जो धर्म को जानता है, किंतु प्रवृत्ति नहीं है, जो पाप को जानता है, किंतु निवृत्ति नहीं है।
फिर महाभारत और उसके बाद का अधिकांश इतिहास ऐसे ही उपाध्यायों का इतिहास है। जब चाणक्य जैसा आचार्य चंद्रगुप्त को उपनीतिकार अध्यापित करता है, तब परिवर्तन होता है। जब कोई समर्थ रामदास शिवा को दीक्षित करता है, तब अन्याय के विरुद्ध तामसिक वृत्तियों के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष प्रारंभ होता है। दीक्षा-गुरु के संदर्भों में विचार करें तो ध्यान में आएगा कि सनातन परंपरा पूर्ववर्ती के साथ उत्तरवर्ती के सातत्य की परंपरा है। मंत्रद्रष्टा ऋषियों से लेकर संतों की वाणी तक सभी जगह एक गुरुक्रम परिलक्षित होता है, अर्थात् शिष्य को
साधना और उपासना के उसी मार्ग की दीक्षा दी गई, जो गुरु को उसकी गुरु-परंपरा से प्राप्त थी। इसलिए तुलसीदास नई भाषा में धर्म का उपदेश देते हुए स्पष्ट रूप से उद्घोष करते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ, वह नाना पुराण निगमागम सम्मत है। भाषा नई है, किंतु आधार पुराने हैं, परंपरा से प्राप्त हैं। शायद इसीलिए विद्रोही तेवर रखनेवाले अघोर संत बाबा किनाराम भी गुरुक्रम को वेदों के मूर्तिमान रूप में ग्रहण करते हैं। यही सांप्रदायिक दीक्षा का शास्त्रीय क्रम है। इसमें युग और व्यक्ति के परिवर्तन के साथ मूल्यों की नित्यता बरकरार रहती है। संप्रदाय का अर्थ ही है, जो पीछे से लेकर आगे की पीढ़ी को दिया जाए।
समकालीन संदर्भों में विचार करें तो गुरु या आचार्य के स्थान पर गुरुडम का विस्तार दिखाई देता है। फलतः आध्यात्मिक जगत् में भी भौतिक उपलब्धि को दिलानेवाले गुरु चमकने लगे। यद्यपि इस क्षेत्र में राज्य का प्रभाव कम होने से सत् मार्ग पर समायोजित करनेवाले लोगों का भी अभाव नहीं है। प्रबल भौतिक प्रभाव के बाद भी विवेकानंद, रामतीर्थ और ऐसे न जाने कितने गुरुओं, संतों के प्रयास चलते रहे। किंतु राज्य सत्ता का प्रभाव सर्वथा अभाव हो ऐसा नहीं है। इसलिए राज्य सत्ता के संबंधों एवं सम्बन्धों के आधार पर चाकचिक्य के द्वारा प्रभामंडल का विस्तार तथा जन समूह को भ्रमित करने की कोशिशें इस युग का यथार्थ है। इस स्थिति में परिवर्तन तभी संभव है जब सनातनता के वास्तविक अर्थ को समझा जाए। यानि नींव पुरानी निर्माण नया कथ्य पुराना भाषा और तर्क नए प्रविधि, नूतन संस्कृति चिर पुरातन के भाव को स्वीकार कर दीक्षा और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में गुरु को सनातन परंपरा में स्थिर किया जाए।
(लेखक, तुलनात्मक धर्म दर्शन के आचार्य एवं पूर्व कुलगुरु हैं।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद