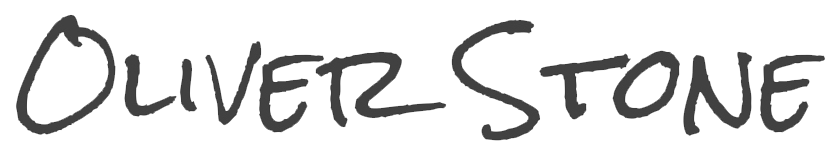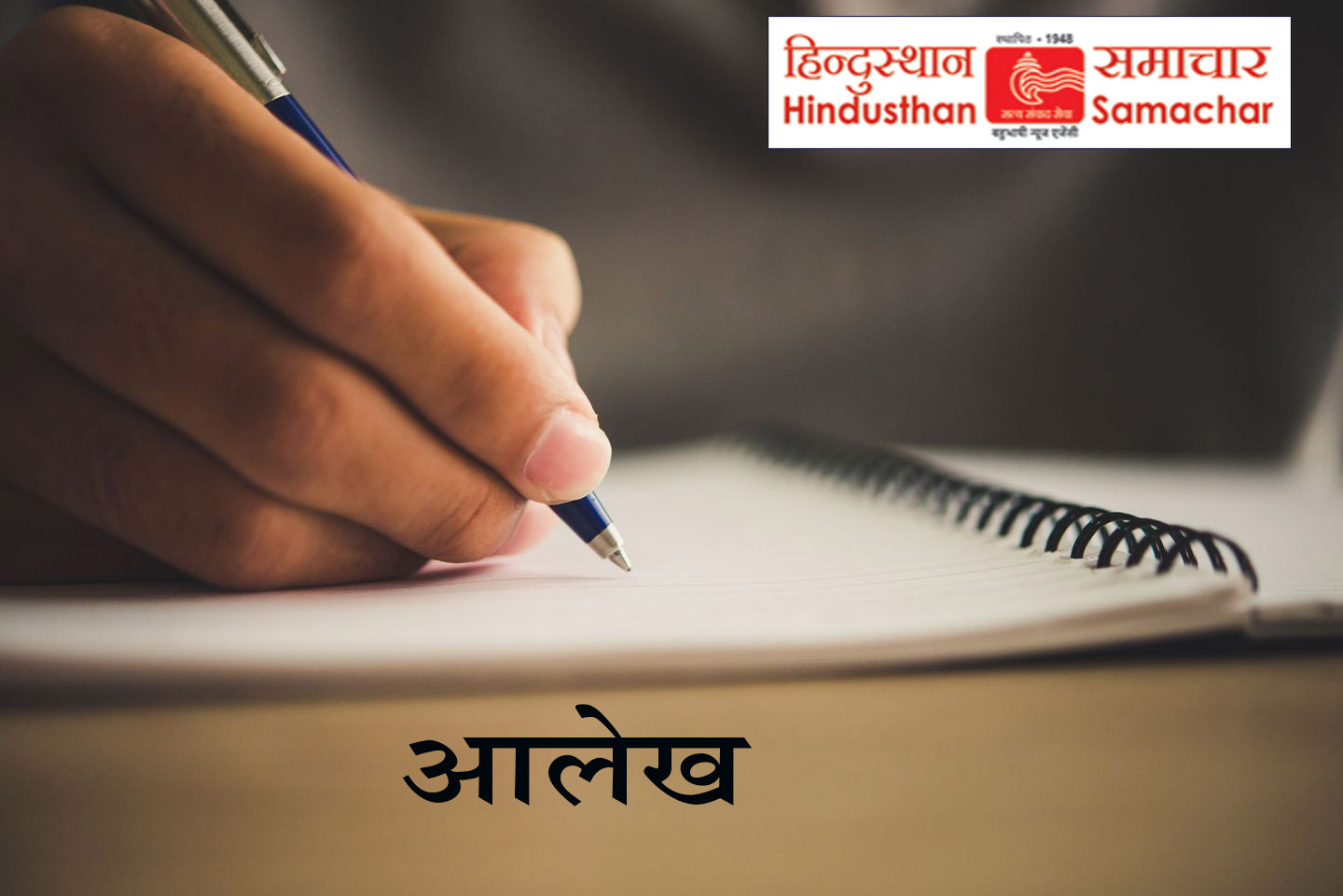Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

हृदयनारायण दीक्षित
दर्शन बुद्धि विलास नहीं है। मानव जीवन को आनंदित करने के लिए दर्शन का सदुपयोग होता रहा है। राष्ट्रीय एकता के लिए भी दर्शन की उपयोगिता है। वेदांत दर्शन का सदुपयोग शंकराचार्य व विवेकानंद ने किया था। वेदांत का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र असाधारण रचना है। इसमें वेदो से लेकर उपनिषद् काल तक विकसित सभी विचारों पर टिप्पणियां हैं। रचनाकार ने सूत्रों में बड़ी-बड़ी बातें की हैं। ब्रह्म सूत्र में पूरी बात के लिए भी अतिअल्प शब्द विन्यास हुआ है। पहला सूत्र है-अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा है। दूसरे सूत्र में दो शब्द ही हैं, ''जन्माद्यस्य यतः। अनुवाद है-यहां जिससे जन्म आदि होते हैं।''
अनुवाद से अर्थ पूरा नहीं निकलता इसलिए अनुभूति की सहायता से कहते हैं-वही ब्रह्म है। अब अर्थ पूरा हुआ ''जिससे जन्म आदि होते है वह ब्रह्म है। 'जन्म आदि' का अर्थ भी बड़ा है - जन्म, युवा, बुढ़ापा, मृत्यु, सृष्टि, स्थिति, विकास और प्रलय। तीसरा सूत्र मात्र एक शब्द का ही है, ''शास्त्रयोनित्वात्''-शास्त्र में वही कारण है। पूरा अर्थ है वह ब्रह्म ही वेदों शास्त्रों में जगत् का कारण कहा गया है। ब्रह्मसूत्रों में सृष्टि जगत का रहस्य है, उपनिषदों में वर्णित तमाम सूत्रों की व्याख्या है।
ब्रह्मसूत्र चार अध्यायों व 16 छोटे-छोटे खण्डों में विभाजित है। 16 खण्डों को पाद-चरण कहा गया है। सूत्रों में वेद उपनिषद् में आए तमाम शब्दों, प्रत्ययों, विचारों का विवेचन है। उपनिषदों में प्राण शब्द आया है। यहां प्राण को ब्रह्म कहा गया है। (1.1.28-31) छान्दोग्य उपनिषद् में सम्पूर्णता के लिए 'भूमा' शब्द आया है। यहां भूमा को ब्रह्म बताया गया है। (1.3.8-9) विवेकानन्द ने भी 'भूमा' को ब्रह्म कहा है 'ब्रह्म' नाना रूपों में परिवर्तित जैसा प्रति भासित होता है। इस प्रकार अद्वैतियों के लिए जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।
उनके अनुसार माया ही जीवात्मा के अस्तित्व का कारण है। पारमार्थिक दृष्टि से उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार सत्ता यदि केवल एक है, तो यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं पृथक सत्ता हूं और तुम एक पृथक् सत्ता हो? यथार्थ में हम लोग सभी एक हैं। हमारी द्वैत दृष्टि ही सभी अनिष्ट का कारण है। जभी मैं यह समझता हूं कि मैं संसार से पृथक् हूं, तभी पहले भय उत्पन होता है और तब दुख का अनुभव होता है। जहां व्यक्ति दूसरे से सुनता है, दूसरे को देखता है, वह अल्प है। जहां व्यक्ति दूसरे को देखता नहीं, दूसरे को सुनता नहीं, वह भूमा है, वह ब्रह्म है। भूमा में परम सुख है, अल्प में नहीं?
सत्य तत्व इन्द्रियों की क्षमता से परे है। सत्य तत्व की व्याख्या वैसे भी कठिन है। श्वेताश्वतर (3.20), कठोपनिषद (2.20) और तैत्तिरीय आरण्यक में एक साथ एक प्यारा सा मंत्र/श्लोक आया है ''अणोरणीयान महतो महीयान-अणु से लघुतम अणु और महान से महत्तर (वह है)''। श्वेताश्वतर (6.19) में इसी बात को और विस्तार देते है ''वह निरवयव है, निश्चल है, शांत, निर्दोष और निर्लिप्त है।''
ब्रह्मसूत्र में 561 सूत्र हैं। सभी सूत्र ब्राह्मणों उपनिषदों का विश्लेषण है। ब्रह्म की स्थापना है। यहां सांख्य दर्शन के कारणवाद का खण्डन है। (अध्याय 2.2.1-10) इसी तरह कणाद के परमाणुवाद से उठे भौतिकवादी प्रश्नों का भी परम ब्रह्म में निरूपण है। (वहीः11-17) बौद्ध और जैनमतों का भी जबर्दस्त खण्डन किया गया है (ब्रह्मसूत्र: गीता प्रेस पृष्ठ 148-177) आगे सारी बाते गीता प्रेस से प्रकाशित ब्रह्मसूत्र की पृष्ठ संख्या के उद्धरणों से लिखी गयी हैं। मधु विद्या अमूल्य है। जैमिनि ने पूर्व मीमांसा में इसे देवताओं के योग्य नहीं बताया क्योंकि देवताओं को यह विद्या सहज प्राप्य है। वे ज्योतिर्मय लोकों में रहते हैं। (पृष्ठ 77 श्लोक 1.3.31-32) अगले श्लोक में लिखा है कि 'वादरायण' को यह मतमान्य नहीं है।
वेद और उपनिषद 'आनंद' को बार-बार दुहराते है। ब्रह्मसूत्र भी 'आनन्दमयो अभ्यसात्' (1.1.12) लिखता है। यहां आनंदमय शब्द में मयट प्रत्यय संसार बोधक है, मय का तात्पर्य 'व्याप्त' होता है, जैसे दुखमय, सुखमय आदि। ब्रह्मसूत्र आनन्दमय को भी ब्रह्मय बताते हैं। लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद में आनंदमय का वर्णन करते हुए उसे सीधे 'रसो वै सः' - वह रस है बताते हैं।
ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों का आनंद भी ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद् में आनंद का विवेचन है। आनंदमय ब्रह्ममयता है। (1.1.12-19) मुण्डकोपनिषद् में एक मंत्र में कहते हैं ''जो अदृश्य है, इन्द्रिय बोध से परे है, वर्णहीन, गोत्रहीन, आंख, कान, पैर से रहित है नित्य, व्यापक, परिपूर्ण और अविनाशी है। धीरपुरूष उसे देखते हैं, वह समस्त भूतों का कारण है। इसी संदर्भ को लेकर ब्रह्मसूत्र में बताया गया है कि वैदिक अनुभूति में जो अदृश्यता आदि गुणों वाला है। वह ब्रह्म है।'' (1.2.21)
ब्रह्मसूत्र मूर्ति पूजा-प्रतीक पूजा की विधि बताता है। आगे कहते हैं 'आसीन सम्भवात्'-बैठकर ही ऐसा सम्भव है। (4.1.7) फिर कहते हैं ''ध्यानाच्य-ध्यान'' (4.1.8) और 'अचलत्वे चापेक्ष्य-शरीर की अचलता की अपेक्षा।'' (4.1.9) ब्रह्मसूत्रों पर तमाम भाष्य लिखे गये। शंकराचार्य का भाष्य अद्वैत सिद्धांत कहलाया। उन्होंने इसी आधार पर ब्रह्म को सत्य और जगत् को मिथ्या बताया।
सबसे दिलचस्प है विद्या का प्रकरण। तीसरे अध्याय के चैथे पाद के प्रथम सूत्र में कहते हैं, ''पुरुषार्थ की सिद्धि इसी से (ज्ञान) होती है। शब्द (वेद) यही बताते हैं।'' अगले सूत्र में कहते हैं कि पूर्व मीमांसा के द्रष्टा आचार्य जैमिनि यह बात नहीं मानते। उनका मत है कि ज्ञान को पुरूषार्थ बताना अर्थवाद है। पुरुषार्थ का साधन तो कर्म हैं। श्रेष्ठजनों के आचरण से यही सिद्ध होता है। छान्दोग्य उपनिषद् में भी कर्म को ही पुरूषार्थ का साधन कहा गया है। कर्म कर्तव्य है। (वही 2-7) 6 सूत्रों में जैमिनी के तर्क बताकर फिर वादरायण का मत है ''श्रुति में कर्म की अपेक्षा विद्या की महत्ता है।'' बड़ी मजेदार लेकिन उचित धारणा है कि विद्या कर्म का भाग नहीं है। अध्ययन कर्म भाग है-अध्ययन मात्रवतः। (वही 3.4.12) बताते हैं कि ''विद्या से कर्मों का (कर्मफल) पूरा नाश हो जाता है।'' (3.4.16)
वैदिक दर्शन में अक्षर शब्द बहुत आया है। वृहदारण्यक उपनिषद् (3.8.7) में अक्षर की विवेचना है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा जो द्युलोक से ऊपर है, पृथ्वी से भी नीचे है। इन दोनो के बीच में भी है। जिसे भूत भविष्य और वर्तमान कहते हैं वह काल किसमे ओत प्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा-आकाश में। गार्गी ने पूछा, वह आकाश किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा उसे ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं, यह न सूक्ष्म है, न लघु, न बड़ा, न लाल, न पीला। ब्रह्मसूत्र (1.3.100) में अक्षर भी ब्रह्म है। सूत्र है ''अक्षरम्बरान्त धृते-अक्षर आकाश पर्यन्त सबको धारण करता है।'' छान्दोग्य उपनिषद् में कहा गया ''निश्चय ही सभी प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते हैं।''
ब्रह्मसूत्र में आकाश भी ब्रह्म है। सृष्टि सृजन के सम्बन्ध में उपनिषदों में अनेक विचार हैं। छान्दोग्य उपनिषद् में तेज, जल और अन्न का क्रमिक विकास है। तैत्तिरीय उपनिषद् में ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति है। फिर आकाश से वायु और वायु से तेज। लेकिन वृहदारण्यक उपनिषद् में आकाश अमृत है। अमृत का जन्म नहीं होता, मरण भी नहीं होता। ब्रह्म सूत्र में सारी शंकाओं, मतों का विवेचन है। फिर ब्रह्म को ही जगत् का कारण बताया गया है। दर्शन का सदुपयोग बौद्ध, जैन ने भी किया, लेकिन शंकराचार्य विरल हैं। उन्होंने राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता को परिपुष्ट किया।
(लेखक, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद