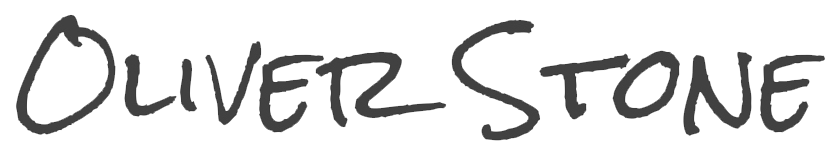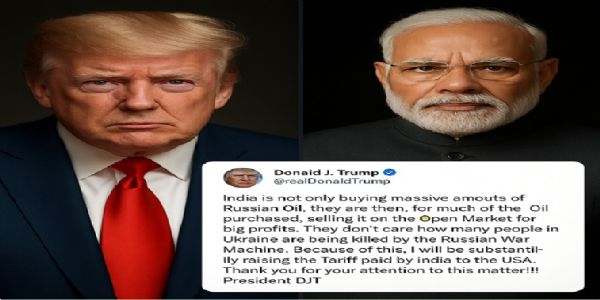Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

रमेश शर्मा
पूरे संसार में अपने पूर्वजों के स्मरण करने और श्रृद्धांजलि अर्पित करने की परंपरा है। लेकिन भारत में अपने पूर्वजों के स्मरण की यह पितृपक्ष की अवधि व्यक्तित्व निर्माण, कुटुम्ब महत्ता और प्रकृति से समन्वय की अद्भुत अवधि है। वस्तुत: भारतीय और पश्चिमी चिंतन में एक आधारभूत अंतर है। पश्चिमी चिंतन केवल वाह्य जगत अर्थात भौतिक सृष्टि तक सीमित है जबकि भारतीय चिंतन लौकिक से अधिक अलौकिक सृष्टि तक व्यापक है। विकास के लिये जितना जोर वाह्य शक्ति और साधनों पर दिया जाता है उससे अधिक आंतरिक ऊर्जा के संचार पर दिया जाता है। इसे हम सनातन परंपरा के सभी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समागमों से समझ सकते हैं और यही विशेषता पूर्वजों के स्मरण के लिये पितृपक्ष के इन दिनों की है।
सूर्योदय से सूर्यास्त तक की पूरी दिनचर्या आंतरिक ऊर्जा जाग्रत करने और आरोग्य शक्ति अर्जित करने की अद्भुत प्रक्रिया है। जबकि इसके कर्मकांड कुटुम्ब समन्वय और प्रकृति से समन्वय बनाकर पर्यावरण संरक्षण के निमित्त हैं। पितृपक्ष की दिनचर्या पर चर्चा करने से पहले इन तीन बिन्दुओं को समझना आवश्यक है । पहली व्यक्ति के अवचेतन की शक्ति, दूसरी आंतरिक ऊर्जा और तीसरी कुटुम्बिक शक्ति एवं ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा और अवचेतन की शक्ति जाग्रत करने के लिये एकाग्रता चाहिए। ऐसी एकाग्रता जिसमें मन के साथ सभी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियों संयुक्त हों।
इसके लिये पितृपक्ष में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय से पूर्व नदी या सरोवर पर स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करने का विधान बनाया गया। घर से नदी या सरोवर जाने में दिवंगत पूर्वजों का स्मरण रहता है। इससे चित्त में एकाग्रता आती है। स्नान करके लौटने में सबका स्मरण बना रहता है। इतनी देर किसी सकारात्मक विचार की एकाग्रता से आत्मशक्ति जाग्रत होती है। यही आत्मशक्ति व्यक्ति पराक्रम और पुरुषार्थ में गुणवत्ता प्रदान करती है। घर आकर पूजन हवन और पाँच ग्रास निकालना मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति, परिवार और प्रकृति से समन्वय का साधन है। इन पांच ग्रास में मछली, चींटी, कौआ, गाय और कुत्ता होते हैं। अर्थात जलचर, थलचर और नभचर तीनों प्रकार के जीवों के संरक्षण का संदेश है।
पितृपक्ष या पितरों की महत्ता का उल्लेख सभी पुराणों में है । श्रीमद्भागवत की रचना ही पूर्वजों की मुक्ति केलिये मानी जाती है। विस्तृत वर्णन गरुण पुराण में है। पितृपक्ष में दिवंगत कुटुम्बजनों का स्मरण करने को श्राद्ध कहा जाता है। श्रृद्धा की केन्द्रीभूत चेतना को श्राद्ध कहा जाता है।सबसे पहले पूर्वजों के प्रतीक के रूप में जौं के आटे का एक छोटा पिण्ड बनाया जाता है। पिण्ड स्थापित करके पितृ गायत्री मंत्र के साथ 108 बार जल अर्पित किया जाता है। पूजन-अर्पण के बाद इस पिण्ड को पीपल के नीचे रखकर अर्पित किये गये जल को किसी बहते जल स्त्रोत में प्रवाहित कर दिया जाता है । फिर कमसे कम एक अभ्यागत अर्थात आमंत्रित अतिथि को भोजन कराने का विधान हैं। यह माना जाता है कि हमारे परिवार जन भले हमारे बीच से विदा हो गये हैं पर उनकी ऊर्जा अवश्य परिवार में रहती है।
पांच ग्रास निकालने का महत्व
इसमें पूजन हवन विधि के बाद महत्वपूर्ण है पांच अलग-अलग प्राणियों के लिये ग्रास निकालना । इनमें गाय, कुत्ता, मछली, चींटी और कौआ हैं। पितरों के संदर्भ इन पांच प्राणियों का जो महत्व पुराणों में वर्णित है उससे अलग इनका समाज और व्यक्तित्व निर्माण से गहरा संबंध है । पितृपक्ष में ग्रास निकालने की परंपरा बनाकर इनका समाज से अटूट रिश्ता बनाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले गाय की महत्ता को देखिये। गाय का दूध हृदयरोग, मधुमेह, कैंसर उपचार में उपयोगी है। गाय का गोबर कृषि के लिये उपयोगी है। गौमूत्र से औषधि तैयार होती है। गाय की श्वांस से हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। इसीलिये भारत के विभिन्न तीज त्योहारों में अलग-अलग माध्यम से गाय को जोड़ा गया और महत्व को स्थापित किया गया है। गाय व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिये तो उपयोगी है ही साथ ही परिवार और समाज की अर्थव्यवस्था में भी बहुत उपयोगी है। इसके साथ गाय के जीवन से व्यक्ति और समाज को सर्व उपयोगी होने और सेवाभाव में जीने का संदेश भी मिलता है । गाय सबसे सरल, सहज और सेवाभावी जीव है। तभी सरल सज्जन और सहनशीलता के लिये गाय का उदाहरण दिया जाता है ।
दूसरा ग्रास कुत्ते के लिये निकाला जाता है। कुत्ता जैसा स्वामी भक्त जीव दूसरा नहीं होता। वह कभी भी पीठ नहीं दिखाता, यदि रणनीति के अंतर्गत वह पीछे हटता है तब भी भौंकता रहता है और अवसर मिलते ही पलटकर हमला करता है। अपने प्राण देकर भी स्वामी की रक्षा करता है। उसकी सूंघने की शक्ति अद्भुत होती है। वह नींद में भी जागरुक रहता है। इसीलिए दत्तात्रेय जी ने कुत्ते को एक आदर्श प्राणी बताया समाज से सदैव सीखने का आव्हान किया। भारतीय मनीषियों ने भी विभिन्न कथाओं के माध्यम से कुत्ते के महत्व को समझाया। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ कुत्ते की स्वर्गारोहण यात्रा सुप्रसिद्ध है । यहां भी पितरों की सेवा को साक्षी बनाकर कुत्ते से परिवार और समाज को जोड़ा गया है ।
पितृपक्ष एवं श्राद्ध में तीसरा ग्रास मछली के लिये निकाला जाता है तथा नदी तालाब में जाकर डाला जाता है। जल किसी भी प्राणी के जीवन का आधार होता है जल की कमी हो या जल अशुद्ध हो तो जीवन संकट में पड़ जाता है और जल का सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत नदी और सरोवर होते हैं। जहाँ मछलियाँ रहतीं हैं। नदी सरोवर या कुँए के जल को शुद्ध रखने का काम मछली करती है । नदी तालाबों में जल को प्रदूषित करने वाले कीटों को मछली अपना आहार बना लेती है । लगता है कि प्रकृति ने जल शुद्धिकरण केलिये ही मछली को बनाया है। अज्ञानता में मनुष्य मछली का कोई अहित न करे इसलिये पितृपक्ष के माध्यम से मछली के संरक्षण को महत्व दिया गया। अलग-अलग पुराण कथाओं में मछली के महत्व को समझाया गया है। मछली के रूप में नारायण के अवतार की कथा भी है। मछली के महत्व को समाज भूले नहीं इसलिये पितृ पूजन से भी मछली को जोड़ा गया। आज भी भारतीय वाड्मय के जानकार लोग मछलियों को दाना डालने जाते हैं।
चौथा ग्रास चींटी के लिये निकाला जाता है। पितृपक्ष में चींटी को भी समाज से जोड़ा गया । आधुनिक विज्ञान के शोध के अनुसार चींटी धरती के पुनर्चक्र को सक्रिय करने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। धरती का यह पुर्नचक्र ही धरती के पोषक तत्वों को पुनर्जीवित करता है। इसी से प्राणियों के जीवन श्रृंखला को निरंतर रहती है। समाज चींटी का संरक्षण करे, इसके लिये विभिन्न कथाओं के माध्यम से समाज को जागरुक किया गया और पितृपूजन से भी जोड़ा। चींटी की सूंघने की शक्ति अद्भुत है । चींटियों में सामाजिक अनुशासन भी है । वे श्रृंखला बद्ध होकर चलतीं हैं। कभी कतार नहीं तोडतीं। कतार को अनुशासित करने केलिये एक टीम चलती है। भोजन खोजने वाली टीम अलग होती है और भोजन ढोकर लाने वाली भी टीम अलग होती है। चीटियों में सामाजिक एकत्व और संगठनात्मक अनुशासन अद्भुत होता है। चींटी से यह संदेश भी है कि भले हमारा अस्तित्व कितना ही लघुतम हो किन्तु मनोबल ऐसा होना चाहिए कि हाथी समान विशालकाय जीव भी भयभीत रहे और संकट आने पर हाथी को भी धराशाई किया जा सके।
पितृपक्ष में पांचवां ग्रास कौए के लिये निकाला जाता है। कौए की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी जीवन शैली सर्वाधिक आत्म अनुशासित है इसीलिए यह सबसे कम बीमार होता है, यह भोजन को देखकर उसमें अशुद्धता भांप लेता है और हानिकारक होने का आभास होते ही ग्रहण नहीं करता। यह भूख से तो मर जाता है पर बीमारी से कभी नहीं मरता। कौए को कभी थकान नहीं होती। कौआ उन विरले प्राणियों में से एक है जो नर और मादा दोनों एक ही आकार के होते हैं। कौये समूह बनाकर रहते हैं। यदि एक साथी कौए को कुछ हो जाये तो दूसरा कौआ साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। इसकी समझ और देखने की सामर्थ्य भी बहुत तीखी होती है । पौराणिक महत्व के अतिरिक्त कौए को समाज से जोड़ने का संदेश यही है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति कुशाग्र हो, दूरदृष्ट हो, समाज संगठित हो।
भारतीय वाड्मय में समाज जीवन में अच्छे व्यवहार की सीख देने वाली अनेक कथाएं हैं पर समाज व्यवहारिक रूप से भी अपने प्रेरणादायकों से जुड़ा रहे। इसलिये पितृपक्ष में इन प्रतीकों के माध्यम से समाज को जाग्रत करने का कर्मकांड निर्धारित किया गया है।
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी