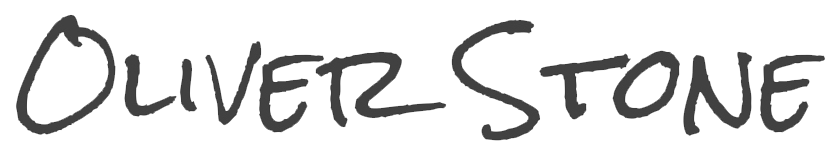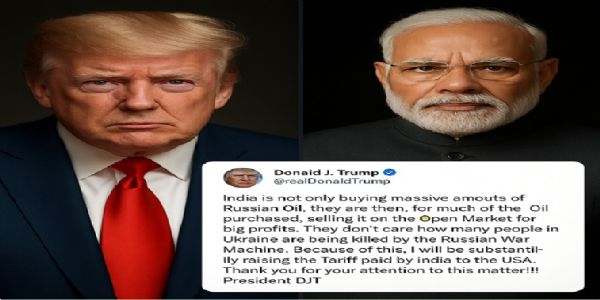Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

-डॉ. जितेंद्र सिंह
एक समय था जब हम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में केवल अनुयायी माने जाते थे, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। भारत न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि वैश्विक साझेदारियों में समान भागीदार बन चुका है। आने वाले वर्षों में गगनयान मिशन और 2035 तक प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, हमारी अंतरिक्ष यात्रा को नई दिशा और नया आयाम देने वाले हैं।
देखा जाए तो यह गगनयान मिशन केवल एक तकनीकी उपलब्धि भर नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। जब हमारे अंतरिक्ष यात्री सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (माइक्रोग्रेविटी) की परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे, तो उसका लाभ पृथ्वी पर भी पहुँचेगा। चाहे वह कृषि हो, जीवन विज्ञान हो या चिकित्सा क्षेत्र, इन प्रयोगों से हमें ऐसे नए निष्कर्ष मिलेंगे जो करोड़ों लोगों के जीवन को आसान बना सकते हैं। हाल के समय में मायोजेनेसिस जैसे प्रयोगों ने भी यह सिद्ध किया है कि अंतरिक्ष अनुसंधान केवल आकाश तक सीमित नहीं, बल्कि धरती पर मानव स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी अहम है। मांसपेशियों के क्षय और पुनर्जनन पर किए गए अध्ययन मधुमेह, कैंसर और फ्रैक्चर जैसी समस्याओं से जूझ रहे रोगियों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं।
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन : 2035 का लक्ष्य
भारत ने 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। हमारा यह लक्ष्य सिर्फ तकनीकी प्रगति तक ही सीमित नहीं है, आज यह राष्ट्रीय संकल्प का भी परिचायक है। जब यह स्टेशन स्थापित होगा तो भारत वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में न केवल साझेदार होगा, बल्कि एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा। इस स्टेशन का महत्व केवल वैज्ञानिक प्रयोगों तक सीमित नहीं रहेगा। यह हमारे सामरिक हितों की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की मजबूती और वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की स्थिति को भी परिभाषित करेगा। प्रधानमंत्री ने “सुदर्शन सुरक्षा चक्र” की जिस परिकल्पना का उल्लेख किया है, उसमें अंतरिक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता
अंतरिक्ष स्टेशन और मानव मिशनों के सफल संचालन के लिए हमें सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर जैसी तकनीकों में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आज दुनिया जान चुकी है कि सेमीकंडक्टर केवल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग तक सीमित नहीं हैं। अंतरिक्ष मिशनों में उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह, एआई आधारित प्रणाली और ऊर्जा संसाधनों का बेहतर उपयोग लंबे समय तक चलने वाले अभियानों के लिए अनिवार्य होगा। यहां यह कहना सही होगा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन केवल धरती पर डिजिटल क्रांति को गति नहीं देगा, बल्कि यह अंतरिक्ष अभियानों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इसी प्रकार, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर न केवल पृथ्वी पर ऊर्जा संकट का समाधान देंगे बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी ऊर्जा स्रोत बनेंगे।
अंतरिक्ष प्रयोग : धरती के लिए लाभकारी
यह एक भ्रम है कि अंतरिक्ष अनुसंधान केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा की तुष्टि के लिए होता है। वास्तविकता यह है कि अंतरिक्ष प्रयोगों के निष्कर्ष सीधे धरती पर मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। लंबे समय तक स्क्रीन के संपर्क के प्रभाव का अध्ययन, माइक्रोग्रेविटी में पौधों की खेती, पुनर्योजी जीव विज्ञान के प्रयोग, ये सभी आज की दुनिया में बेहद प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, माइक्रोग्रेविटी में मेथी उगाने के प्रयोग न केवल अंतरिक्ष यात्रियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, बल्कि यह कृषि अनुसंधान के लिए भी नई दिशा देंगे। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और खाद्य संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब ऐसे प्रयोगों का महत्व और भी बढ़ जाता है।
अंतरिक्ष का व्यावसायिक और आर्थिक आयाम
भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लगभग 400 स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। ये स्टार्टअप्स न केवल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि मैपिंग, स्मार्ट सिटी विकास, कृषि, टेलीमेडिसिन और उपग्रह संचार जैसे क्षेत्रों में भी नवाचार ला रहे हैं। सरकार ने हाल ही में 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड मंजूर किया है, जो इन स्टार्टअप्स को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में मदद करेगा। अंतरिक्ष अब युवाओं के लिए आकर्षक करियर विकल्प बन चुका है। एक समय था जब एयरोस्पेस इंजीनियरिंग को केवल एक विशिष्ट शाखा माना जाता था, लेकिन आज यह आईआईटी जैसे संस्थानों में सबसे अधिक मांग वाला विषय बन चुका है।
सुरक्षा और कूटनीति का नया युग
भारत ने आने वाले पाँच वर्षों में 52 जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है। यह योजना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज युद्ध केवल जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतरिक्ष भी उसका अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उपग्रहों से मिली जानकारी हमारी सामरिक तैयारी को मजबूत करती है और सीमा पर तैनात सैनिकों को वास्तविक समय में मदद पहुँचाती है। ऐसे में इन-स्पेस जैसी संस्थाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के बावजूद सुरक्षा से कोई समझौता न हो। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर इस क्षेत्र को उदार बनाया गया है, लेकिन साथ ही कड़े विनियमन भी बनाए रखे गए हैं। यह संतुलन ही भारत को नवाचार और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर सफल बनाता है।
अंतरराष्ट्रीय सहयोग और प्रतिस्पर्धा
यहां हम सभी के लिए यह भी ध्यान देने योग्य है कि आज जब चीन अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर चुका है और अमेरिका-रूस दशकों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, ऐसे समय में भारत का प्रवेश केवल वैज्ञानिक महत्व का नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक दृष्टि से भी निर्णायक है। गगनयान मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हमें अंतरराष्ट्रीय मानवयुक्त मिशनों में सहभागी बनाएंगे। आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष पर्यटन का भी दौर शुरू होने वाला है। जैसे-जैसे यह क्षेत्र व्यवहार्य होगा, भारत के पास डॉकिंग, सर्विसिंग और पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्यात करने का अवसर होगा। इससे न केवल हमारी तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ेगी, बल्कि विदेशी मुद्रा अर्जन के नए रास्ते भी खुलेंगे।
हमारा लक्ष्य स्पष्ट है
भारत ने 2033 तक वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में आठ प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है। फिलहाल हमारी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग आठ अरब डॉलर की है, लेकिन अगले दशक में इसके 40-45 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। यह वृद्धि न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को नई गति देगी, बल्कि हमें विश्व मंच पर एक सशक्त खिलाड़ी भी बनाएगी। गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रमा पर मानव मिशन और निजी-सरकारी साझेदारी से उभरती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, ये सभी भारत को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहाँ से वह विश्वगुरु बनने की दिशा में एक और निर्णायक कदम बढ़ा सकेगा।
भारत का अंतरिक्ष भविष्य केवल विज्ञान या तकनीक तक सीमित नहीं है। यह हमारे आत्मविश्वास, हमारी युवा शक्ति, हमारी महिला वैज्ञानिकों और हमारी सामूहिक आकांक्षा का प्रतिबिंब है। आज हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में भारत की सबसे बड़ी पहचान उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम ही होगा। यही वह क्षेत्र है, जो हमें न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि वैश्विक स्तर पर नेतृत्व दिलाएगा।
(लेखक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) , विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी