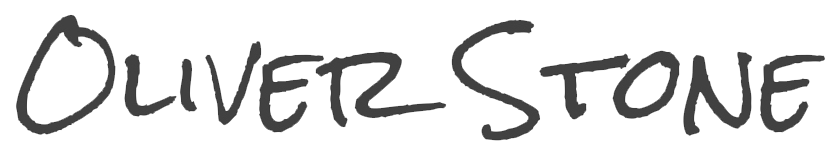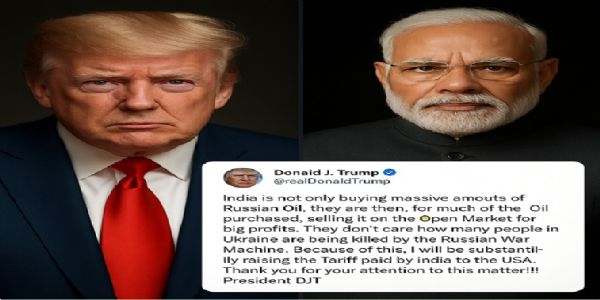Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

-डॉ. निवेदिता शर्मा
विश्व शेर दिवस, जो प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है, केवल वन्यजीव प्रेमियों का एक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर स्मरण है कि धरती पर जीवन की विविधता को बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम शेर की बात करते हैं, तो हमारे मानसपटल पर सबसे पहले उभरती है उसकी शान, उसका गौरव और उसकी अदम्य शक्ति, जिसे सदियों से ‘जंगल का राजा’ कहा जाता रहा है। किंतु इस उपाधि के पीछे का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक हो सकता है, जब हम यह सुनिश्चित करें कि यह राजा अपने प्राकृतिक क्षेत्र में सुरक्षित और समृद्ध बना रहे। भारत के संदर्भ में यह चर्चा और भी प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि यहां एशियाई शेर की एकमात्र आबादी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है, जो पूरी दुनिया में अद्वितीय है।
एशियाई शेर एक समय पूरे एशिया, मध्य-पूर्व और भूमध्यसागरीय क्षेत्र में फैले हुए थे। किंतु मानव विस्तार, शिकार और आवासीय क्षरण ने इनके विस्तार को लगातार सीमित किया, और 20वीं सदी की शुरुआत तक यह प्रजाति केवल काठियावाड़ के गिर जंगलों तक सिमट गई। किंतु आज उनकी संख्या बढ़ने के समाचार उत्साहवर्धक कहे जा सकते हैं, वर्ष 2020 में 674 की तुलना में मई 2025 में इनकी अनुमानित संख्या 891 तक पहुंच गई है, जो लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि है। यह उपलब्धि निस्संदेह गुजरात सरकार, वन विभाग, ‘प्रोजेक्ट लायन’ और स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी प्रजाति के संरक्षण की यात्रा में केवल संख्या वृद्धि ही सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता, उनके लिए स्थायी और सुरक्षित आवास, मानव-वन्यजीव संघर्ष का समाधान और जीन-पूल की विविधता का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है।
गुजरात में शेर केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान तक सीमित नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनका प्राकृतिक विस्तार बढ़कर सौराष्ट्र के 11 जिलों में लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर में फैल चुका है। यह क्षेत्रीय प्रसार दोहरा संदेश देता है कि गिर का पारंपरिक आवास अब शेरों की बढ़ती संख्या को समेटने में सक्षम नहीं रहा। वहीं, आज यह भी बता रहा है कि शेर प्राकृतिक रूप से नए इलाकों को अपनाने में सक्षम है, बशर्ते वहां पर्याप्त शिकार और पानी की उपलब्धता हो। इसी संदर्भ में बरदा वन्यजीव अभयारण्य का महत्व बढ़ जाता है, जो पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिलों में 192.31 वर्ग किलोमीटर में फैला है और अब एशियाई शेरों का दूसरा घर बनकर उभर रहा है। 2023 में शेरों के प्राकृतिक प्रवास के बाद यहां की संख्या 17 तक पहुंच गई, जिनमें 6 वयस्क और 11 शावक शामिल हैं। यह विकास केवल एक पारिस्थितिक घटना नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि यदि हम उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध कराएं, तो शेर स्वयं अपने अस्तित्व के लिए नए रास्ते तलाश सकते हैं।
वास्तव में बरदा का महत्व केवल शेर संरक्षण तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र एक समृद्ध जैव-विविधता हॉटस्पॉट है, जहां विभिन्न वनस्पतियां, पक्षी और अन्य वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका द्वारका–पोरबंदर–सोमनाथ पर्यटन सर्किट के निकट होना, इसे न केवल संरक्षण के दृष्टिकोण से बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी एक अवसर बनाता है। लगभग 248 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित सफारी पार्क इसी दिशा में एक कदम है, जिससे न केवल वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि नियंत्रित और जिम्मेदार पर्यटन से स्थानीय समुदायों को भी आर्थिक लाभ होगा। राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन और लगभग 180 करोड़ रुपये के संरक्षण कार्यों की शुरुआत इस बात का संकेत है कि नीति-निर्माण अब संरक्षण को विकास के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
फिर भी, शेर संरक्षण की राह चुनौतियों से मुक्त नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है मानव-वन्यजीव संघर्ष। जैसे-जैसे शेरों का विस्तार कृषि क्षेत्रों और मानव बस्तियों के निकट हो रहा है, वैसे-वैसे मवेशियों के शिकार, लोगों की सुरक्षा और फसल क्षति जैसे मुद्दे बढ़ रहे हैं। इसका समाधान केवल क्षतिपूर्ति योजनाओं या वन विभाग के त्वरित हस्तक्षेप से संभव नहीं है; इसके लिए दीर्घकालिक सामुदायिक सहभागिता और सह-अस्तित्व की रणनीतियां जरूरी हैं। ग्रामीण समुदायों को यह महसूस कराना कि शेर केवल खतरा नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान का हिस्सा हैं, एक कठिन लेकिन आवश्यक कार्य है। गुजरात में कई गांवों ने इसे अपनी परंपरा और गर्व के रूप में अपनाया है, लेकिन यह भावनात्मक जुड़ाव सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकसित करना होगा।
एक और गंभीर मुद्दा है जीन-पूल की सीमित विविधता। चूंकि पूरी एशियाई शेर आबादी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित है, इसलिए किसी भी महामारी, प्राकृतिक आपदा या बड़े पैमाने पर आवासीय क्षति से पूरी प्रजाति को खतरा हो सकता है। विशेषज्ञ लंबे समय से सुझाव दे रहे हैं कि शेरों की एक दूसरी स्थायी आबादी किसी अन्य राज्य या भौगोलिक क्षेत्र में बसाई जाए, ताकि जोखिम का बंटवारा हो सके। इस दिशा में कई योजनाएं बनीं, लेकिन राजनीतिक, प्रशासनिक और स्थानीय प्रतिरोध के कारण वे अब तक मूर्त रूप नहीं ले पाईं। बरदा का विकास इस समस्या का आंशिक समाधान हो सकता है, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से हमें राज्य की सीमाओं से बाहर भी सोचने की आवश्यकता है।
जलवायु परिवर्तन भी शेर संरक्षण के भविष्य में एक अनदेखा लेकिन बड़ा कारक है। बदलते मौसम पैटर्न, पानी के स्रोतों पर दबाव और चरागाहों की गुणवत्ता में गिरावट दीर्घकाल में शेरों के शिकार आधार को प्रभावित कर सकती है। यदि हिरण, नीलगाय और अन्य शिकार प्रजातियों की संख्या घटेगी, तो शेरों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना कठिन हो जाएगा। इसलिए, शेर संरक्षण को केवल ‘शेर बचाओ’ कार्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय, इसे एक समग्र पारिस्थितिक प्रबंधन के रूप में देखना होगा, जिसमें शिकार प्रजातियों का संरक्षण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और घासभूमियों का पुनर्निर्माण शामिल हो।
यहां यह उल्लेखित है कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एशियाई शेर भारत के वन्यजीव कूटनीति का भी प्रतीक हैं। जैसे अफ्रीकी हाथी या पांडा चीन के वन्यजीव विरासत के प्रतीक हैं, वैसे ही एशियाई शेर भारत की वैश्विक छवि में गर्व का स्थान रखते हैं। भारत का यह दायित्व है कि वह इस प्रजाति के संरक्षण में न केवल घरेलू स्तर पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भी योगदान दे। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजीस्) में भूमि पर जीवन और जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्य स्पष्ट हैं, और शेर संरक्षण उनमें सीधा योगदान देता है। साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी शेर पर्यटन गुजरात के लिए एक स्थायी आय स्रोत है। गिर राष्ट्रीय उद्यान हर वर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, और इसके साथ जुड़े होटल, गाइड, परिवहन और स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। यदि बरदा और अन्य क्षेत्रों का संरक्षण-आधारित विकास किया जाए, तो यह मॉडल पूरे देश में अपनाया जा सकता है।
कहना होगा कि आज जब हम विश्व शेर दिवस मना रहे हैं, तो यह अवसर है प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य का जीवंत प्रतीक के लिए। शेर की दहाड़ में केवल शक्ति का स्वर नहीं, बल्कि प्रकृति की उस जटिल श्रृंखला की प्रतिध्वनि है, जिसका हिस्सा हम भी हैं। यदि यह दहाड़ कभी थम गई, तो इसका अर्थ होगा कि हमने अपने पारिस्थितिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ खो दिया है। इसलिए, शेर संरक्षण को केवल वन विभाग या सरकारी योजनाओं की जिम्मेदारी न मानकर, इसे लोक के स्वभाव का अंग बनाना बनाना होगा। विद्यालयों में बच्चों को शेर और उनके आवास के बारे में शिक्षित करना, स्थानीय समुदायों को संरक्षण के लाभ समझाना, और शहरी समाज को भी वन्यजीव-हितैषी जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना उतना ही जरूरी है जितना कि वैज्ञानिक शोध या वित्तीय निवेश।
अंततः यही कहा जाए तो उचित होगा कि एशियाई शेर का भविष्य हमारे सामूहिक निर्णयों पर निर्भर करेगा। क्या हम उसे केवल एक स्मृति, एक चित्र या एक प्रतीक में सिमटने देंगे या यह सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी दहाड़ को सुन सकें? विश्व शेर दिवस का वास्तविक संदेश यही है कि आओ; हम खुद से यह संकल्प लें कि ‘जंगल का राजा’ हमेशा अपने साम्राज्य में सुरक्षित और स्वतंत्र रहेगा और उसके साथ-साथ हमारी धरती की जैव-विविधता भी हम सभी के बीच सदैव अपने विस्तार को आगे बढ़ाती रहेगी ।
(लेखिका, जैव विविधता की अध्येता एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी