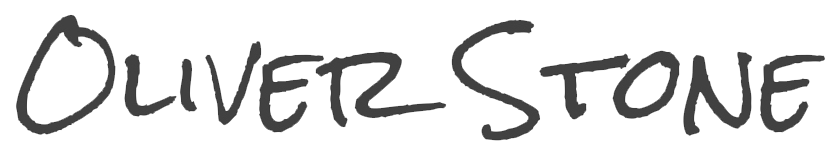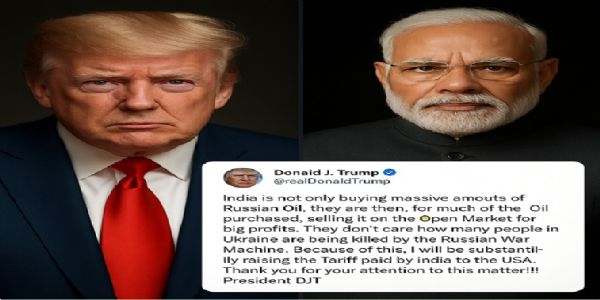Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

-डॉ. मयंक चतुर्वेदी
इस वर्ष भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1,50,590 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है। इस तरह भारत के रक्षा औद्योगिक इतिहास में नया अध्याय लिख गया है। यह केवल एक रिकॉर्ड तोड़ संख्या नहीं, बल्कि उस परिवर्तन का प्रतीक है जिसकी नींव पिछले एक दशक में रखी गई और जिसे अब ठोस परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। वास्तव में यह राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक सामर्थ्य के क्षेत्र में भारत के दीर्घकालिक प्रयासों की परिणति है। पिछले वर्ष के 1.27 लाख करोड़ रुपये के उत्पादन की तुलना में यह 18 प्रतिशत की सशक्त वृद्धि है, जबकि 2019-20 के 79,071 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत की छलांग है, जो यह दर्शाती है कि भारत ने रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में कितनी तेज़ी से प्रगति की। यह तथ्य है कि 2019-20 के 79,071 करोड़ रुपये की तुलना में 90 प्रतिशत की विस्मयकारी छलांग है। इन आँकड़ों के पीछे पिछले दशक में अपनाई गई नीतियों, सुधारों और निवेशों की पूरी श्रृंखला है, जिसने भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर रक्षा उत्पादन विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स), अन्य सार्वजनिक निर्माताओं और निजी उद्योग के सभी हितधारकों की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने इसे भारत के मजबूत होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत बताया है। वस्तुत: यह कथन केवल औपचारिक प्रशंसा नहीं है, बल्कि एक नीतिगत घोषणा भी है कि भारत का रक्षा उद्योग अब एक ऐसे स्तर पर पहुँच चुका है जहाँ वह न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि निर्यात में भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा कर सकता है।
अब जरा उत्पादन में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिकाओं पर नज़र डालें तो तस्वीर और स्पष्ट होती है। डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (डीपीएसयू) और अन्य सार्वजनिक उपक्रम कुल उत्पादन का लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23 प्रतिशत तक पहुँच चुका है। यह आँकड़ा एफवाई 2023-24 में 21 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि निजी उद्योग की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। यह वृद्धि केवल प्रतिशत में नहीं, बल्कि वास्तविक उत्पादन में भी दिखती है; एफवाई 2024-25 में निजी क्षेत्र के उत्पादन में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में यह 16 प्रतिशत रही। इसका अर्थ है कि निजी उद्योग न केवल रक्षा विनिर्माण में अधिक निवेश कर रहा है, बल्कि उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में भी तेजी से प्रगति कर रहा है।
यदि हम थोड़ा पीछे जाएँ तो स्थिति इतनी आशाजनक नहीं थी। 2014-15 में भारत का कुल रक्षा उत्पादन लगभग 77,000 करोड़ रुपये के आसपास था। उस समय देश की रक्षा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता था। रूस, फ्रांस, अमेरिका, और इज़राइल जैसे देशों से हथियार, मिसाइल, विमान और नौसैनिक उपकरण बड़ी मात्रा में खरीदे जाते थे। घरेलू निर्माण मुख्यतः कुछ सीमित हथियार प्रणालियों और उपकरणों तक ही सीमित था और उनमें भी उच्च तकनीकी घटक विदेशों से आयात किए जाते थे। किंतु हम देखते हैं कि वर्ष 2016 के बाद से इस क्षेत्र में परिदृश्य बदलना शुरू हुआ। ‘मेक इंन इण्डिया’ पहल के तहत रक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई और निजी उद्योग को इसमें प्रवेश देने के लिए नीतिगत दरवाज़े खोले गए। 2017-18 में कुल उत्पादन 84,000 करोड़ रुपये के आसपास पहुँच गया, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ 2020 में आया, जब ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र को आयात प्रतिस्थापन के स्पष्ट लक्ष्य दिए गए। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी-2020) और रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति (डीपीईपीपी-2020) ने उद्योग को दिशा और स्थिरता दी।
इन नीतियों के तहत ‘नकारात्मक आयात सूची’ जारी की गई, जिसमें दर्ज सैकड़ों उपकरणों और हथियारों को भविष्य में केवल भारत में ही निर्मित करने का प्रावधान किया गया। यह कदम न केवल विदेशी निर्भरता कम करने की दिशा में था, बल्कि घरेलू उद्योग को स्थायी बाज़ार सुनिश्चित करने वाला भी साबित हुआ। साथ ही, श्रजन पोर्टल के माध्यम से विदेशी उपकरणों के स्वदेशी विकल्प विकसित करने के प्रयास तेज़ हुए।
आज जब हम 2024-25 के आँकड़ों को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि ये नीतिगत कदम परिणाम दे रहे हैं। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और अन्य सार्वजनिक निर्माता कुल उत्पादन का लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत तक पहुँच गई है, जो 2023-24 में 21 प्रतिशत थी। यह परिवर्तन मामूली नहीं है, क्योंकि निजी क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि 28 प्रतिशत रही है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में यह 16 प्रतिशत रही।
आज देखने में आ रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में एचएएल, बीईएल, बीडीएल, एमडीएल, जीआरएसई जैसी कंपनियाँ अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने तो बहुत कम समय में बड़ा काम करके दिखा दिया है, उसने तेजस हल्के लड़ाकू विमान, ध्रुव हेलिकॉप्टर और रुद्र अटैक हेलिकॉप्टर का निर्माण किया है। इसी तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने राडार, संचार उपकरण और आकाश वायु रक्षा प्रणाली में अपनी क्षमता साबित की है। निजी क्षेत्र में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा डिफेंस और अदानी डिफेंस जैसी कंपनियाँ अब मिसाइल लांचर, आर्मर्ड व्हीकल, नौसैनिक जहाज़ और एयरोस्पेस कंपोनेंट्स का निर्माण कर रही हैं।
यही कारण है कि आज रक्षा निर्यात के मोर्चे पर भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 2014-15 में यह आँकड़ा मुश्किल से 1,500 करोड़ रुपये के आसपास था। 2016-17 में यह 1,522 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,682 करोड़ रुपये हुआ। 2018-19 में यह 10,745 करोड़ रुपये और 2022-23 में 15,920 करोड़ रुपये तक पहुँचा। 2023-24 में यह 21,083 करोड़ रुपये और अब 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर है। यह वृद्धि न केवल आयात पर निर्भरता घटाती है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत को एक रक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करती है।
एक एक उत्साह से भर देनेवाला आंकड़ा है; भारत अब 90 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। इनमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के कई देश शामिल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को निर्यात, रक्षा कूटनीति का एक सफल उदाहरण है। आने वाले वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुँचाना है। इसके लिए हथियार प्रदर्शनियों, द्विपक्षीय रक्षा समझौतों, सस्ते वित्तपोषण और रक्षा अटैशे नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। हालाँकि, इन सफलताओं के बावजूद चुनौतियाँ कम नहीं हैं। उन्नत इंजन तकनीक, जेट इंजन, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कुछ विशेष सामग्री के लिए अभी भी विदेशी आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता बनी हुई है। अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम है, जबकि दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा के लिए यही वह क्षेत्र है जो निर्णायक साबित होता है।
इसके अलावा, परियोजनाओं के समय पर पूरा होने, लागत नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने की चुनौतियाँ भी हैं।किंतु यदि मौजूदा नीतिगत गति और औद्योगिक निवेश की प्रवृत्ति बनी रही, तो 2029 तक भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपये और रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपये के पार पहुँच सकता है। उस स्थिति में भारत न केवल आत्मनिर्भर होगा, बल्कि मित्र देशों के लिए भी भरोसेमंद रक्षा आपूर्ति स्रोत बनेगा।
कहना होगा कि यह केवल आर्थिक लाभ का मामला नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक प्रभाव और रणनीतिक स्वायत्तता को भी मजबूत करेगा।इसलिए, 2024-25 का यह रिकॉर्ड केवल अतीत की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर ही नहीं देता है, बल्कि भविष्य की तैयारी का आह्वान भी करता है। आत्मनिर्भर भारत का रक्षा क्षेत्र अब वैश्विक मानचित्र पर अपनी जगह बना चुका है, अगला कदम इसे शीर्ष पर पहुँचाना है। इसके लिए सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थान और सेना को मिलकर उस दृष्टि को साकार करना होगा, जिसमें भारत न केवल अपने लिए, बल्कि दुनिया के लिए भी सुरक्षा का स्तंभ बन सके। यही वह भविष्य है जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं और जिसकी बुनियाद आज के इन आँकड़ों ने और मजबूत कर दी है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी