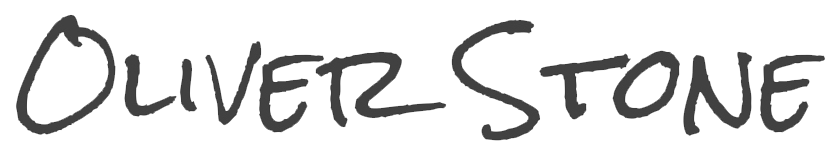Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

गिरीश्वर मिश्र
हर कोई अपने लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना चाहता है ताकि हर स्थिति का मुकाबला किया जा सके और इस बात की दौड़ लगी रहती है कि थोड़ा और हो जाता तो अच्छा होता। पर पर्याप्त की मरीचिका आगे-आगे भागती है और हम पीछा ही करते रहते हैं। आम आदमी की जिंदगी में अकसर ऐसी परिस्थिति आती रहती है जब सामने कोई नए मॉडल का फोन या कार, शर्ट या बैग या फिर कुछ भी नया लिए सजा-धजा दिखता है। इसे देख हमें भी लगता है कि वह सब मेरे पास भी हो । एक बार मेरे सामने भी एक युवा एक नए मॉडल के फोन के साथ फोटो खींच रहा था। मेरे मन में भी हिलोर उठी और मुझे लगा कि मेरे पास भी यह फोन होना चाहिए । फिर मैंने अपनी इच्छा पर किसी तरह काबू पाया। मेरे पास दो साल बाद भी आज अपना पहले वाला ही फोन है और वह ठीक काम कर रहा है और मैं खुश भी हूं । अब एक दूसरी घटना लीजिए । पिछले साल मैंने एक आई पैड खरीदा । सोचा था इससे लिखने-पढ़ने का काम और अच्छी तरह और सुविधापूर्वक कर सकूँगा । पर आई पैड के आने के बाद मेरे काम धाम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ज्यादातर समय वह आई पैड पड़ा ही रहा और मैं अपने पुराने लैपटाप से ही काम करता रहा। आई पैड को दो एक बार पोंछ-पाछ कर चार्ज जरूर किया था।
ये महंगा था और अपने खर्चों में किसी तरह कतर-ब्योंत कर ही इसे खरीद पाया था। दरअसल नया फोन, नया सोफा, नया जूता या फिर कोई भी नई चीज लेने के बाद हफ्ते भर बीतते न बीतते वह चीज साधारण, बासी और पुरानी लगने लगती है। तब फिर हम उसे अपने उपयोग में नहीं लाते। ऐसा होने के बाद उसके लिए हमारी इच्छा की तीव्रता भी कम होने लगती है, वह ढलने लगती है । साथ ही बहुतेरी इच्छाओं के बीच से चुनने का अतिभार जैसा भी होने लगता है। हमारे सामने सवाल है कि इसे कैसे कम किया जाय या किफ़ायती कैसे बना जाय ? हमारे मस्तिष्क की पुरस्कार प्रणाली को अधिक जीवंत और संतोषप्रद कैसे बनाया जाय ? “थोड़ा और” की प्रवृत्ति बताती है कि हमारा मस्तिष्क नए-नए संसाधनों को इकट्ठा करने में जुटा रहता है। आदिम मनुष्य के जीवन में भोजन इकट्ठा करने और दीर्घ जीवन के लिए यह युक्ति कारगर थी । आज के दौर में पुरस्कार की जगह बदलाव और अप्रत्याशित फायदे हमें अधिक आकर्षित करते हैं। इस व्यवस्था ने हमारे पूर्वजों को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वे ‘बस थोड़ा सा और’ पाने की जुगत में ही उलझे रहें । तब यह निश्चित ही उपयोगी था क्योंकि इससे वे अस्पष्ट और अनिश्चय की स्थिति में भी जीवन यापन कर सके थे । सुरक्षा की दृष्टि से यह जरूरी था।
आज की बात कुछ और है। हमारी दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब वैसी असुरक्षा और अनिश्चय की स्थिति नहीं रही। ‘थोड़ा और’ अर्जित करने के अवसर अब हम पुराने माडल को अपग्रेड करने और अन्य चीजों के विकल्पों में बदल चुके हैं। इस बदली परिस्थिति में हम लोग जो कुछ हमारे पास पहले से है उससे जो ज़्यादा है या बढ़-चढ़ कर है उसे चाहने लगते हैं। यह नियति का खेल है कि एक समय जिस बात ने जीवन को खुशहाल बनाया था वह अब बेकार की फ़िज़ूलखर्ची और भयानक असंतोष के दुष्चक्र को जन्म दे रही है। यह तरीका उस दौर के लिए था जब परिवेश में असुरक्षा थी और उपलब्ध साधन सीमित थे। आज के अतिशय और अतिरेक के दौर के लिए वह मौजू नहीं रहा । आज सामाजिक मीडिया का भी तेजी से उभार है। हम सब लगातार किसी को अपने से अलग कुछ और करते या खरीदते देखते हैं। इस तरह का अनुभव करते हुए हम ख़ुद को बड़ा मजबूर महसूस करने लगते हैं।
हमारे लिए ‘पर्याप्त’ का आशय उस चीज को पाने से होता है जो हमारे पास मौजूद चीज से बाहर होता है । ऐसे में “कुछ और” या “थोड़ा और” कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता । इच्छाओं के अनुकूलन की प्रवृत्ति के चलते आदमी जल्दी ही एक स्थिर ख़ुशी के स्तर पर वापस लौट आता है। ‘थोड़ा और’ कभी भी पर्याप्त इसलिए नहीं लगता कि हम इच्छाओं के अनुकूलन के शिकार होते रहते हैं। यानी हमारी प्रवृत्ति है कि हम बहुत जल्द एक अपेक्षाकृत स्थायी सुख के सामान्य स्तर पर आ टिकते हैं। जीवन में बड़ी सकारात्मक या ऋणात्मक घटना के बाद जैसे लाटरी या अशक्तता का ख़ुशी या दुख पर सिर्फ़ क्षणिक प्रभाव होता है। हम फिर वापस अपने सामान्य स्तर पर वापस आ जाते हैं। यह अनुकूलन हमारी प्रतिरोध क्षमता को तो सुदृढ़ करता है पर नई उपलब्धि के रोमांच का आकर्षण तेजी से घटने लगता है। प्रत्याशा बढ़ी तो यह ऊँचा होता है और धीरे-धीरे सामान्य अवस्था पर लौट आता है। हमारा ध्यान नई ख़रीद की ओर आकर्षित होने लगता है और अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का क्रम चल पड़ता है। फिर एक नया चक्र शुरू हो जाता है। आज की उपभोक्ता संस्कृति में अपग्रेड, नए विकल्प, और अनुकूलन, से उपजा असंतोष लगातार बना रहता है।
मजेदार बात यह है कि अगली चीज का अनुभव होने पर या अपग्रेड करने के लिए निवेश करने का लाभ लगातार घटता जाता है। आदमी सोचता है कि अगर फलाँ चीज होती तो ख़ुशी मिलती । नई ख़रीद से उत्तेजना होती है पर वह जल्दी ही मुरझाने लगती है । अपग्रेड करते ही आपको लगता है कि नया संस्करण या नया मॉडल चाहिए। ऐसा लगने में ज़्यादा देर नहीं लगती । वस्तुओं की ख़रीदी सूची कुछ और है जो संतोष के लिए जरूरी चीजों की सूची कुछ और। संतोष देने की जगह नई ख़रीददारी अगली चीज के चाहने पर जोर देती है। चुनाव का यह अजीब विरोधाभास है कि विकल्प बढ़ने के क्रम में पहले तो अच्छा लगता है पर एक मुकाम यह भी आता है जब अधिक विकल्प होना हमें कम संतुष्ट करने लगता है। हम सोचते हैं कि हमें विकल्प चाहिए और लगता है कि अधिक से अधिक चीजें पाने पर हम सुखी हो सकेंगे । पर वस्तुत: होता उल्टा है। कई अध्ययन बताते हैं कि ज्यादा संख्या में विकल्प का होना चुनने की थकान को बढ़ाता है। चुनाव का बहुत ज्यादा अवसर चुनने से मिलने वाली हमारी संतुष्टि की मात्रा को घटाता है । अत्यधिक विविधता हमको पंगु बनाती है न कि समृद्ध या शक्तिसंपन्न ।
न्यूनीकरण या किफ़ायत करना जीने का दूसरा रास्ता है जिसमें अति को छोड़ कर हम चीजों को सरल करते हैं । तब कम सीमाएँ बनती हैं जो हमारी बौद्धिक, संज्ञानात्मक, सांवेगिक संसाधनों की रक्षा करती हैं। थोड़े विकल्प हमारी इच्छा-शक्ति को सुदृढ़ करते हैं और निर्णय की चुनौती को कम करते हैं। तब हम सिर्फ़ सार्थक लक्ष्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं । जब नवीनतम को पीछे छोड़ते हैं विकल्पों की बाढ़ कम करते हैं तो हम जो अपने पास है उस पर ध्यान देते हैं और समझदारी के साथ खर्च करते हैं। हमारी ख़ुशी को वस्तुओं की प्राप्ति से कम जानबूझ कर थोड़े या कम को चुन निरन्तर भूख के कोलाहल को कम करने पर अधिक आनंद मिलता है । ऐसे में पुरस्कार लुप्त नहीं होता है। इसके बदले जो है उसका अनुभव या आस्वादन हमारे अनुकूलन को कम कर सकता है।
खरीदने के पहले प्रतीक्षा करना ठीक है न कि उतावली में खरीदना । किफायती दृष्टि होने पर बेज़रूरी चीज़ों की भीड़ तथा निर्णय लेने की थकान भी कम होती है। हम अवसर पा सकेंगे ताकि यात्रा, सीखने, सामाजिक कार्य में जुट कर ख़ुशी का अनुभव कर सकें। ‘अति’ को मना कर समय और ऊर्जा के लिए हम ‘हां’ करते हैं। वस्तुओं को छोड़ने से पश्चाताप की जगह अपनी पहचान बनाते हैं । अधिक का पीछा कभी भी सुखी नहीं बना सकता । किफायतीपन वस्तुत: एक व्यावहारिक विकल्प है । स्वेच्छया शांति, अपनी खुशी से न कि बाहरी दबाव या सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण चुनने से खुशी बढ़ती है और तनाव कम होता है । जरूरी है हम सूचना के अतिभार से बचें। भय और दूसरों से प्रतिपुष्टि की जगह आनंद और आंतरिक संतुष्टि को महत्व देना चाहिए। अपनी अनुभूतियों और वर्तमान क्रियाओं पर ध्यान देते हुए जो है उससे प्रसन्न होना चाहिए न कि जो नहीं है उसे लेकर चिंतित हों । इसके लिए सोशल मीडिया के उपयोग की सीमा बांध कर उन चीजों के लिए मना करना होगा जो आपके किसी काम की न हों। उन चीजों में लगें जो आपको प्रसन्न करती हैं यानी पढ़ना, सृजन या कहीं मन लगाना। आख़िर पर्याप्त कोई संख्या नहीं होती है, वह हमारी सोच है।
(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं।)
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद