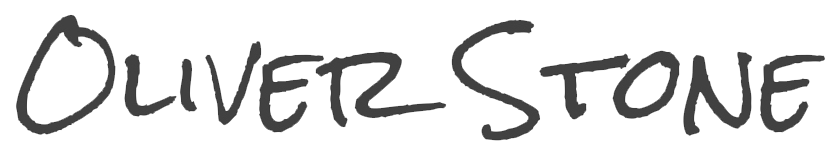Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

डॉ. मयंक चतुर्वेदी
भारत का राजनीतिक परिदृश्य एक बार फिर वैचारिक बहस के केंद्र में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल का हवाला दिया, जिससे देशभर में राजनीतिक हलचल देखी गई । गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी ओर कहा, आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है, जिसने करोड़ों युवाओं को राष्ट्रसेवा और समाज निर्माण की दिशा दिखाई है।
वस्तुत: खरगे का बयान ऐसे समय आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक दौर में हैं। कांग्रेस का यह कदम चुनावी राजनीति के संदर्भ में समझा जा रहा है। वह चुनावी लाभ के लिए आरएसएस के बहाने भाजपा को चुनावी सफलता से दूर रखना चाहती है। यदि इतिहास में जाकर इस मामले की समीक्षा करें तो स्थिति स्वत: ही पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। आरएसएस पर प्रतिबंधों का इतिहास यह है कि संगठन पर स्वतंत्र भारत में अब तक तीन बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है और दो बार कांग्रेस की सरकार के दौरान वापस भी लिया गया।
तथ्य यह है कि पहला प्रतिबंध 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगा। नाथूराम गोडसे के संघ से जुड़ाव के संदेह के आधार पर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने संगठन को बैन किया। करीब 17,000 स्वयंसेवक जेल भेजे गए और संघ की शाखाएँ बंद कर दी गईं। किंतु बाद में जांच में यह स्पष्ट हुआ कि गांधीजी की हत्या में संघ का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ नहीं। सरदार पटेल ने स्वयं 27 फरवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर स्वीकार किया कि “गांधी हत्या के आरोपों में से 90 प्रतिशत अटकलों और झूठी बातों पर आधारित हैं।” बाद में जुलाई 1949 में सरकार ने बिना किसी शर्त के संघ से प्रतिबंध हटा लिया। स्वयं पटेल ने लिखा, “संघ पर से प्रतिबंध हटने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है।” यह तथ्य कांग्रेस के उस दावे को कमजोर करता है, जिसके आधार पर आज फिर से संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है।
दूसरा प्रतिबंध 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने लगाया। उस समय संघ लोकतंत्र बहाली के लिए विपक्ष के साथ खड़ा था। 21 महीनों तक हजारों स्वयंसेवक जेलों में रहे, लेकिन जब जनता ने 1977 में इंदिरा सरकार को सत्ता से बाहर किया, तो संघ का जनाधार पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरा। तीसरा प्रतिबंध दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद लगा। लेकिन अदालतों में सरकार संघ के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं रख सकी। कुछ महीनों में यह प्रतिबंध भी हट गया। इन तीनों घटनाओं ने एक बात स्पष्ट कर दी कि प्रतिबंध संघ को कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि वह कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे भारतीय संविधान का उल्लंघन होता है।
सरदार पटेल और संघ का वास्तविक संबंध
कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने सरदार पटेल का हवाला देकर संघ के खिलाफ बयान दिया, लेकिन इतिहास इसके विपरीत गवाही देता है। पटेल और संघ के तत्कालीन सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) के बीच संवाद कायम था। 16 जुलाई 1949 को पटेल ने वेंकटराम शास्त्री को पत्र लिखकर कहा था, “मैं स्वयं प्रतिबंध हटाने के पक्ष में था।” संघ से प्रतिबंध हटने के बाद उन्होंने गुरुजी को पत्र लिखकर अपनी खुशी प्रकट की। यह वही पटेल हैं जिन्होंने सलाह दी थी कि “यदि आरएसएस को लगता है कि कांग्रेस गलत दिशा में जा रही है, तो सुधार का रास्ता भीतर से निकालिए, विरोध से नहीं।”
इस संवादशील दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल संघ के राष्ट्रसेवी चरित्र को समझते थे, भले ही विचारों में मतभेद रहे हों। ऐसे में आज जब कांग्रेस उन्हीं पटेल का नाम लेकर संघ पर प्रतिबंध की मांग करती है, तो यह ऐतिहासिक तथ्यों के आधे-अधूरे उपयोग का उदाहरण बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह देश की जनता को गुमराह कर रही है।
आरएसएस का कार्यक्षेत्र राजनीति से परे समाज के बीच सेवा के रूप से व्यापक तौर पर फैला हुआ है। शिक्षा, ग्राम विकास, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता में संघ का योगदान बहुत विस्तारित है। 1962 के चीन युद्ध में स्वयंसेवकों ने सीमाओं पर सैनिकों की मदद की और इसी सेवा भाव से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में संघ को भाग लेने का निमंत्रण दिया। यह तथ्य आज के राजनीतिक विवादों के बीच अक्सर भुला दिया जाता है।
सीधे तौर पर जो दिखाई दे रहा है, वह यही है कि कांग्रेस को भय है कि संघ की बढ़ती सामाजिक स्वीकार्यता उसकी पारंपरिक वोटबैंक राजनीति के लिए चुनौती है। उसे लगता है कि वह तमाम जाति भेद उभारने, एक वर्ग विशेष को लेकर तुष्टीकरण करने के बाद भी यदि सफल नहीं हो पा रही है तो इसके लिए कहीं न कहीं आरएसएस के स्वयंसेवक जिम्मेदार हैं, जो हर परिस्थिति में भारत के जन की एकता पर जोर देते हैं। इसलिए समय-समय पर आरएसएस पर प्रतिबंध या उसकी आलोचना कांग्रेस के लिए वैचारिक एकजुटता का साधन बन जाती है। किंतु इस सब के बीच एतिहासिक तथ्य यही कहते हैं कि ऐसे हर प्रयास जो संघ को रोकने के लिए किए जाते हैं, उसमें हर स्तर पर आरएसएस और सशक्त होकर ही सभी के सामने आया है।
यहां आरएसएस के सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के कहे शब्दों पर भी गौर करना सही होगा, उन्होंने खरगे की मांग को “अवास्तविक और इतिहासविहीन” बताया है। उनका साफ कहना है कि किसी संगठन पर प्रतिबंध केवल इच्छा या असहमति के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) जैसे कानूनों के तहत तभी कार्रवाई संभव है जब संगठन हिंसा, आतंक या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल पाया जाए। संघ के मामले में ऐसा कोई आरोप या सबूत नहीं है। संघ के संदर्भ में समाज और न्यायपालिका दोनों ने पहले भी इस तरह के प्रतिबंधों को गलत माना है। वास्तव में, संघ अब केवल संगठन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का पर्याय बन चुका है। 1948, 1975 और 1992 के प्रतिबंध इस तथ्य के साक्ष्य हैं कि आरएसएस को दबाने की कोशिशें हर बार विफल हुईं।
अत: मल्लिकार्जुन खरगे का बयान सही तथ्यों पर आधारित नहीं है, वह एक राजनेता हैं और यहां भी सिर्फ वे अपने लाभ के लिए स्वार्थ की राजनीति ही कर रहे हैं। क्योंकि सरदार पटेल ने कहा था, “संघ को कांग्रेस से मतभेद हो सकता है, पर उसका देशभक्ति से कोई विरोध नहीं।” यह वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना साल 1949 में था। उन्हें यह समझना होगा कि राजनीति में असहमति आवश्यक है, पर राष्ट्रसेवा के भाव को संदेह के घेरे में रखना लोकतांत्रिक चेतना के विपरीत है। कहना होगा कि संघ से असहमति रखने का अधिकार सबको है लेकिन उसके योगदान को नकारना इतिहास की सच्चाई से आँखें मूँद लेने जैसा होगा। संघ का मूल विचार यही है, “देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें।”
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. मयंक चतुर्वेदी